
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 4
April 2025
Indexing Partners
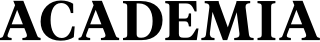




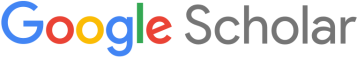













बौद्ध शिक्षा प्रणालीः आधुनिक एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता
| Author(s) | राजेंद्र मीणा, डॉ चंद्रशेखर शर्मा |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | बौद्ध शिक्षा प्रणाली विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध शैक्षिक परंपराओं में से एक रही है। यह केवल ज्ञान के अर्जन तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्म-साक्षात्कार, नैतिकता, और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित थी। बौद्ध शिक्षा ने बौद्ध मठों, विहारों और शिक्षा केंद्रों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया। यह अध्ययन बौद्ध शिक्षा की पारंपरिक अवधारणा, उसके ऐतिहासिक विकास, समय के साथ हुए परिवर्तनों और आधुनिक संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करेगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता इसका व्यावहारिक और समावेशी दृष्टिकोण था। यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, गणित और व्याकरण जैसे विषयों का भी समावेश किया गया था। इस शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक और नैतिक उत्थान के साथ-साथ समाज में शांति, अहिंसा और सद्भाव की स्थापना करना था। इसके लिए शिक्षा को अनुभवजन्य, संवाद-आधारित और नैतिक मूल्यों से युक्त बनाया गया था, जिससे न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक विकास को भी बल मिला। इतिहास गवाह है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। इन शिक्षा केंद्रों में न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। बौद्ध शिक्षा ने इन क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी और वहां की स्थानीय शिक्षा प्रणालियों को प्रभावित किया। इसने ज्ञान के अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया, जिससे यह प्रणाली न केवल भारत तक सीमित रही बल्कि वैश्विक बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ, बौद्ध शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से विदेशी आक्रमणों और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान शिक्षण संस्थान विध्वंस के शिकार हुए, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि, बौद्ध धर्म और इसकी शिक्षा प्रणाली ने तिब्बत, श्रीलंका, जापान और अन्य देशों में पुनर्जीवित होकर नई ऊर्जा प्राप्त की। आज, आधुनिक शिक्षण प्रणालियों में बौद्ध शिक्षा के तत्वों का समावेश देखा जा सकता है, विशेष रूप से ध्यान (माइंडफुलनेस), नैतिक शिक्षा, और समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में। आधुनिक संदर्भ में बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता को देखते हुए, इसकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, नैतिकता, और शांति अध्ययन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। माइंडफुलनेस और ध्यान आधारित चिकित्सा पद्धतियाँ, जो बौद्ध परंपराओं से प्रेरित हैं, आज वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा, वर्तमान समय में कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बौद्ध अध्ययन को औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे इसकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षा प्रणाली की परंपरा, उसमें समय के साथ हुए परिवर्तन, और आधुनिक समय में इसकी भूमिका को व्यापक रूप से समझना है। यह शोध इस बात का विश्लेषण करेगा कि किस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज भी समाज को प्रभावित किया है और इसके मूल तत्व आज के वैश्विक शिक्षण परिदृश्य में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। बौद्ध शिक्षा की परंपरा बौद्ध शिक्षा की परंपरा अत्यंत समृद्ध और व्यापक थी, जो न केवल आध्यात्मिक उत्थान बल्कि बौद्धिक और नैतिक विकास पर भी केंद्रित थी। इसकी नींव गौतम बुद्ध के शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित थी, जो चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति, ध्यान और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करती थी। इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर विशेष बल दिया जाता था, जिससे वह न केवल अपने स्वयं के मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान दे सके। प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से संचरित होती थी। बुद्ध के उपदेश उनके शिष्यों द्वारा स्मरण किए जाते थे और उन्हें अनुशासनबद्ध रूप में आगे बढ़ाया जाता था। बौद्ध संघों और विहारों में शिक्षा का प्रमुख माध्यम संवाद और श्रवण पर आधारित था, जहाँ गुरु-शिष्य परंपरा का विशेष महत्व था। शिक्षा का मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार और व्यक्ति में नैतिक शुद्धता एवं आत्मज्ञान को बढ़ावा देना था। बौद्ध ग्रंथों को समय के साथ पालि, संस्कृत और अन्य भाषाओं में लिपिबद्ध किया गया, जिससे बौद्ध शिक्षा को संरक्षित और विस्तारित करने में सहायता मिली। त्रिपिटक (विनय पिटक, सुत्त पिटक, और अभिधम्म पिटक) बौद्ध शिक्षा के मूल ग्रंथों में शामिल हैं, जो न केवल धार्मिक शिक्षाओं बल्कि नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। इन ग्रंथों में ध्यान, आत्मसंयम, शील (नैतिकता), और प्रज्ञा (बुद्धिमत्ता) जैसे गुणों पर बल दिया गया है, जो किसी भी शिक्षण प्रणाली के मूलभूत तत्व माने जाते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में महाविहारों और विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी और सोमपुर जैसे महान शिक्षा केंद्रों ने बौद्ध शिक्षा को व्यापक स्तर पर प्रसारित किया। इन संस्थानों में केवल धार्मिक अध्ययन ही नहीं, बल्कि दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, शिल्पकला, और अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, जहाँ न केवल भारत से बल्कि चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। इन महाविहारों में शिक्षा प्रणाली अत्यंत संगठित थी और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश की एक निश्चित प्रक्रिया थी। विद्यार्थी अपने गुरु के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते थे और बौद्ध ग्रंथों को कंठस्थ करने के साथ-साथ बौद्ध तर्कशास्त्र एवं ध्यान अभ्यास में भी संलग्न रहते थे। शिक्षक और शिष्य के मध्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ और अनुशासनबद्ध होते थे, जहाँ शिक्षकों की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी देखा जा सकता है। चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कोरिया में बौद्ध शिक्षा ने गहरा प्रभाव डाला और वहाँ के स्थानीय शिक्षा ढांचे में इसका समावेश हुआ। तिब्बत में बौद्ध शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया और वहाँ बौद्ध ग्रंथों के विस्तृत अनुवाद हुए। चीन में फा-ह्यान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने भारत आकर नालंदा और अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को अपने देश में ले जाकर अनुवादित किया, जिससे बौद्ध शिक्षा चीन में भी विकसित हुई। बौद्ध शिक्षा की परंपरा ने वैश्विक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित किया। यह शिक्षा प्रणाली केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित न रहकर एक व्यापक दार्शनिक, वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। इसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं, जहाँ ध्यान (माइंडफुलनेस), करुणा, अहिंसा और समता जैसे सिद्धांत आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी अपनाए जा रहे हैं। इस प्रकार, बौद्ध शिक्षा की परंपरा न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक संदर्भों में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। इसकी शिक्षाएँ आज भी जीवन में नैतिकता, अनुशासन, और मानसिक शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं, जिससे यह शिक्षा प्रणाली एक वैश्विक धरोहर के रूप में स्थापित हो चुकी है। समय के साथ हुए परिवर्तन बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने समय के साथ विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के कारण कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना किया। प्रारंभिक काल में यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली और सुव्यवस्थित थी, लेकिन समय के साथ इसमें कई उतार-चढ़ाव आए। विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और बौद्ध विचारधारा के विकास ने इसकी संरचना और प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित किया। 1. महायान और हीनयान बौद्ध शिक्षा का विकास बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रारंभिक चरण में थेरेवाद (हीनयान) पर अधिक बल दिया जाता था, जो मूल रूप से आत्मसंयम, ध्यान और व्यक्तिगत मोक्ष की साधना पर केंद्रित थी। इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और बौद्ध संघ (संघ समुदाय) के अनुशासन का पालन करना था। किन्तु, समय के साथ महायान बौद्ध विचारधारा का विकास हुआ, जिसने बौद्ध शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। महायान परंपरा ने बोधिसत्व मार्ग को अपनाया, जिसमें न केवल आत्मज्ञान, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने को प्राथमिकता दी गई। इस विचारधारा के प्रभाव से बौद्ध शिक्षा में अधिक दार्शनिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक विषयों को शामिल किया गया, जिससे यह एक बहुआयामी शिक्षा प्रणाली बन गई। तिब्बती बौद्ध शिक्षा प्रणाली, जो महायान परंपरा का प्रमुख केंद्र बनी, ने ग्रंथों के विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। 2. शिक्षा केंद्रों का पतन प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने चरम पर थी, लेकिन समय के साथ यह कई बाहरी आक्रमणों और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कमजोर होती गई। विशेष रूप से 12वीं शताब्दी में तुर्क और मुस्लिम आक्रमणों के कारण नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और वल्लभी जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध शिक्षा केंद्र नष्ट हो गए। इन संस्थानों के विनाश से बौद्ध शिक्षा प्रणाली को भारी क्षति पहुँची, और भारत में इसकी प्रभावशीलता धीरे-धीरे कम हो गई। इसके अलावा, मध्यकालीन भारत में हिंदू पुनर्जागरण और भक्ति आंदोलन के प्रभाव के कारण बौद्ध शिक्षा को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। इस दौरान बौद्ध शिक्षा केंद्रों का स्थान ब्राह्मणवादी गुरुकुल और इस्लामिक मदरसों ने लेना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, बौद्ध शिक्षा का प्रभाव दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों में अधिक दिखाई देने लगा, जबकि भारत में यह धीरे-धीरे सीमित होती गई। 3. पुनरुद्धार और आधुनिक पुनर्योजना 19वीं और 20वीं शताब्दी में बौद्ध शिक्षा के पुनरुद्धार का एक नया दौर शुरू हुआ। विशेष रूप से, डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए प्रयासों ने भारत में बौद्ध विचारधारा को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दलित वर्गों को सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की दिशा में प्रेरित करने के लिए बौद्ध शिक्षा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, आधुनिक काल में थेरवाद और महायान बौद्ध समुदायों द्वारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली को पुनः संगठित करने का प्रयास किया गया। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान और तिब्बत में बौद्ध विश्वविद्यालयों और अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे बौद्ध शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पुनः पहचान मिली। वर्तमान समय में बौद्ध शिक्षा को आधुनिक विज्ञान, दर्शन, और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन के लिए विशेष विभाग स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और उनका आधुनिक संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। भारत में भी नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के प्रयास किए गए हैं, जिससे बौद्ध शिक्षा प्रणाली को पुनः सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने समय के साथ अनेक महत्वपूर्ण बदलावों का सामना किया है। प्रारंभ में यह आत्मज्ञान और नैतिकता पर केंद्रित थी, लेकिन महायान परंपरा के विकास के साथ यह अधिक समावेशी बन गई। मुस्लिम आक्रमणों और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसका भारत में पतन हुआ, लेकिन आधुनिक काल में इसके पुनरुद्धार के प्रयास किए गए। आज बौद्ध शिक्षा प्रणाली केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शिक्षण पद्धति के रूप में उभर रही है, जो शांति, नैतिकता, और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आधुनिक संदर्भ में बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, मानसिक संतुलन, नैतिक मूल्यों की स्थापना, और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना भी हो गया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा की शिक्षाएँ विभिन्न स्तरों पर प्रासंगिक साबित हो रही हैं, क्योंकि यह केवल धार्मिक या दार्शनिक विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव समाज, मनोविज्ञान, और पर्यावरणीय चेतना पर भी देखा जा सकता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं में किया जा सकता है: 1. नैतिक शिक्षा और अनुशासन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा की भूमिका कमजोर होती जा रही है, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन की गिरावट देखी जा रही है। बौद्ध शिक्षा का मूल आधार करुणा, अहिंसा और सत्य जैसे नैतिक सिद्धांतों पर टिका हुआ है, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली छात्रों को केवल बौद्धिक रूप से विकसित करने पर बल नहीं देती, बल्कि उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने की दिशा में भी प्रेरित करती है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को पुनः लागू करने के लिए बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों में सहानुभूति, ईमानदारी, और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो। 2. ध्यान (माइंडफुलनेस) और मानसिक स्वास्थ्य आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, अवसाद, और चिंता जैसी समस्याएँ आम हो गई हैं। आधुनिक चिकित्सा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बौद्ध ध्यान (मेडिटेशन) तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। बौद्ध माइंडफुलनेस (सचेतनता) तकनीक, जिसे विशेष रूप से पश्चिमी देशों में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, आज शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का भाग बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त, योग और ध्यान की प्रथाएँ मानसिक तनाव को कम करने, आत्म-जागरूकता को बढ़ाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बौद्ध शिक्षा के इन तत्वों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध शिक्षाएँ आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। 3. समावेशी और वैश्विक शिक्षा बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत समावेशिता और समानता पर आधारित था। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, विक्रमशिला, और तक्षशिला में भारत के साथ-साथ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वर्तमान वैश्विक शिक्षा प्रणाली में समावेशिता और बहुसंस्कृतिवाद पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बौद्ध शिक्षा के इन सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा में शामिल कर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों के छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करे। इसके अलावा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू गैर-हिंसक संवाद और सामाजिक समरसता पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्षों और सांस्कृतिक विभाजनों के बीच बौद्ध शिक्षा के सिद्धांत शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। 4. पर्यावरणीय चेतना और सतत विकास बौद्ध दर्शन और शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को न केवल जीवों के प्रति, बल्कि संपूर्ण प्रकृति के प्रति अपनाने का संदेश दिया था। आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए, बौद्ध शिक्षा का यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बौद्ध शिक्षा के मूल सिद्धांतों को अपनाना आज के समाज की प्राथमिक आवश्यकता बन चुकी है। विभिन्न देशों में बौद्ध समुदाय और संस्थान पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, थाईलैंड और म्यांमार में बौद्ध मठों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और जापान में ज़ेन बौद्ध परंपरा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य कर रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इन सिद्धांतों को सम्मिलित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। 5. बौद्ध शिक्षण संस्थानों का पुनरुद्धार आधुनिक समय में कई देशों ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और तिब्बत में भी बौद्ध अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई है, जहाँ पारंपरिक बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बौद्ध अध्ययन और दर्शन पर विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहाँ छात्र बौद्ध ग्रंथों, ध्यान पद्धतियों, और बौद्ध विचारधारा पर गहन अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही, डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर बौद्ध शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रचारित किया जा रहा है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली केवल प्राचीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह आज भी सामाजिक, मानसिक, नैतिक और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। नैतिक शिक्षा, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, समावेशिता, और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में बौद्ध शिक्षा के सिद्धांतों की प्रासंगिकता आधुनिक समय में और भी बढ़ गई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यदि बौद्ध शिक्षा के मूल तत्वों को समाहित किया जाए, तो एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था विकसित की जा सकती है जो न केवल बौद्धिक विकास पर केंद्रित हो, बल्कि समाज में नैतिकता, शांति, और सतत विकास को भी बढ़ावा दे। ऐसे प्रयासों से न केवल प्राचीन बौद्ध परंपराओं का संरक्षण होगा, बल्कि यह एक आधुनिक, समावेशी, और संतुलित शिक्षा प्रणाली के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली केवल धार्मिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज और व्यक्ति के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। इसके सिद्धांत नैतिकता, अनुशासन, शांति, सह-अस्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, जिसमें सामाजिक अस्थिरता, मानसिक तनाव और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, बौद्ध शिक्षा के मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यदि बौद्ध दृष्टिकोण को समाहित किया जाए, तो यह नैतिक एवं समावेशी शिक्षा को सशक्त बना सकता है। माइंडफुलनेस, करुणा, और आत्मअनुशासन जैसे सिद्धांत शिक्षा को केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित न रखकर जीवन कौशल विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम बना सकते हैं। इसके साथ ही, पर्यावरणीय चेतना और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी बौद्ध शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मूल्यों को पुनः स्थापित करें और इसे समकालीन संदर्भों में लागू करने के लिए प्रभावी नीतियाँ विकसित करें। इसके लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बौद्ध नैतिकता, ध्यान तकनीकों, और सामाजिक समरसता पर आधारित शिक्षाओं को शामिल करना एक सार्थक कदम हो सकता है। इस दिशा में सही प्रयासों से हम एक संतुलित, नैतिक और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान दे सकते हैं। संदर्भ 1. अमृत कुमार, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली: प्रकाशन भारती, 2015, पृष्ठ 102-115। 2. राहुल सांकृत्यायन, बौद्ध शिक्षा का ऐतिहासिक विश्लेषण, वाराणसी: ज्ञानपीठ प्रकाशन, 2010, पृष्ठ 85-98। 3. डी.एन. झा, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय: नालंदा और तक्षशिला का योगदान, कोलकाता: ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008, पृष्ठ 45-60। 4. तारा नाथ, बौद्ध शिक्षा केंद्रों का पतन और पुनरुत्थान, पटना: बिहार राष्ट्रीय प्रकाशन, 2017, पृष्ठ 150-165। 5. एच.जी. रॉलेनसन, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा, लंदन: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1922, पृष्ठ 78-95।आनंद, एस. (2015). बौद्ध शिक्षा का ऐतिहासिक विकास और आधुनिक प्रासंगिकता. वाराणसी: संस्कृत प्रकाशन। 6. तिवारी, आर. (2018). प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली: नालंदा और तक्षशिला का योगदान. दिल्ली: ज्ञान भारती पब्लिकेशन। 7. धम्मानंद, के. (2019). बौद्ध धर्म और शिक्षा: परंपरा से आधुनिकता तक. बोधगया: बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। 8. अंबेडकर, भीमराव. (1956). बुद्ध और उनका धम्म. नागपुर: सिद्धार्थ कॉलेज पब्लिकेशन। 9. Gethin, R. (1998). The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University Press. 10. Lopez, D. S. (2001). The Story of Buddhism: A Concise Guide to Its History & Teachings. HarperOne. 11. Rahula, W. (2006). What the Buddha Taught. New York: Grove Press. 12. Thera, N. (2014). Buddhist Education and Monastic Tradition. Bangkok: Buddhist Studies Press. 13. त्रिपाठी, एम. (2020). भारतीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा का योगदान. प्रयागराज: राष्ट्रीय पुस्तकालय। 14. Keown, D. (2013). Buddhism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 3, March 2025 |
| Published On | 2025-03-03 |
| Cite This | बौद्ध शिक्षा प्रणालीः आधुनिक एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता - राजेंद्र मीणा, डॉ चंद्रशेखर शर्मा - IJLRP Volume 6, Issue 3, March 2025. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

