
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 4
April 2025
Indexing Partners
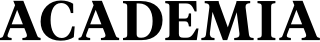




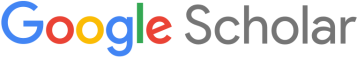













राजस्थान में कृषि का आर्थिक प्रगति में योगदान का भौगोलिक विश्लेषण
| Author(s) | Prem Shankar Kirar |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, विविध प्राकृतिक परिस्थितियों और जलवायु विशेषताओं वाला क्षेत्र है। राज्य का बड़ा भाग शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, जहाँ वर्षा की अनिश्चितता और पानी की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि एक कठिन कार्य बन जाती है। यहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है, और जल संकट, मृदा की उर्वरता में गिरावट, तथा जलवायु परिवर्तन जैसे कारक इसके विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद, राजस्थान की कृषि न केवल खाद्य उत्पादन बल्कि आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। राजस्थान की कृषि का स्वरूप इसकी भौगोलिक विविधता से प्रभावित होता है। राज्य में जैसलमेर और बाड़मेर जैसे अति-शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ कृषि अत्यंत सीमित है, वहीं कोटा और भरतपुर जैसे क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक उपजाऊ हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, मूंगफली और कपास हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सब्जियाँ, औषधीय पौधे और मसाले भी व्यापक रूप से उगाए जाते हैं। साथ ही, राजस्थान पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है और इसे 'भारत का ऊन भंडार' भी कहा जाता है। पशुपालन न केवल कृषि आधारित आय का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि यह ग्रामीण आजीविका का भी महत्वपूर्ण अंग है। राज्य की कृषि में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी सिंचाई योजनाओं का भी विशेष योगदान रहा है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के बंजर क्षेत्रों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा ‘राजस्थान कृषि नीति’ और ‘मुख्यमंत्री कृषि सुधार योजना’ जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि, सिंचाई सुविधाओं की कमी, आधुनिक कृषि तकनीकों का सीमित उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और किसानों की आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इस शोध पत्र में राजस्थान की कृषि का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है, जिसमें इसकी विशेषताओं, आर्थिक प्रभाव, चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह अध्ययन राजस्थान की कृषि को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सहायक होगा और इसके सतत विकास के लिए प्रभावी नीतियों को प्रस्तावित करने में योगदान देगा। राजस्थान की कृषि की विशेषताएँ राजस्थान की कृषि विविध भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें जलवायु, मृदा की विशेषताएँ, सिंचाई सुविधाएँ और कृषि उत्पादन की विविधता प्रमुख हैं। राज्य में कृषि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. जलवायु का प्रभाव: राजस्थान मुख्यतः शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 100 मिमी से 800 मिमी तक होती है, जो क्षेत्र विशेष के अनुसार भिन्न होती है। पश्चिमी भागों में, जैसे जैसलमेर और बाड़मेर, वर्षा अत्यधिक सीमित होती है, जिससे कृषि में जल संकट बना रहता है। पूर्वी राजस्थान में, जैसे कोटा और भरतपुर, वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे यहाँ अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। वर्षा की अनिश्चितता और मानसूनी विसंगतियाँ कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे सूखा और जल-संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। 2. मिट्टी के प्रकार: राजस्थान में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है। • रेतीली मिट्टी: यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और जलधारण क्षमता कम होने के कारण सिंचाई पर अधिक निर्भर होती है। • लाल एवं काली मिट्टी: पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और अनाज व तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। • जलोढ़ मिट्टी: चंबल, बनास और घग्घर नदी के किनारे यह मिट्टी पाई जाती है, जो अधिक उपजाऊ होती है और गेहूँ, गन्ना और सब्जियों की खेती के लिए अनुकूल होती है। • मरुस्थलीय मिट्टी: पश्चिमी राजस्थान में यह मिट्टी लवणीयता और क्षारीयता से प्रभावित होती है, जिससे कृषि उत्पादकता सीमित हो जाती है। 3. फसलों की विविधता: राजस्थान में विभिन्न प्रकार की खाद्य, नकदी और तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। • खरीफ फसलें: बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास और ग्वार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। • रबी फसलें: गेहूँ, चना, सरसों, जौ और धनिया प्रमुख रबी फसलें हैं। • नकदी फसलें: राजस्थान में कपास, गन्ना, जीरा, सौंफ और मेथी जैसी नकदी फसलों की भी महत्वपूर्ण खेती होती है। • औषधीय एवं मसाला फसलें: अजवाइन, अश्वगंधा, एलोवेरा और इसबगोल जैसी औषधीय फसलों की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। 4. सिंचाई प्रणाली: राजस्थान में सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर करता है। हालाँकि, कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ कृषि को सहारा देने का कार्य कर रही हैं: • इंदिरा गांधी नहर परियोजना: यह पश्चिमी राजस्थान में कृषि के विस्तार में सहायक रही है और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में योगदान दिया है। • जवाई बांध: पाली और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। • भूजल पर निर्भरता: राजस्थान में सिंचाई के लिए मुख्य रूप से भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है, जिससे जल स्तर में गिरावट हो रही है। • कृत्रिम जल संचयन: राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन प्रणालियाँ, जैसे बावड़ियाँ, तालाब और कुंड, कृषि जल प्रबंधन में सहायक रही हैं, लेकिन इनका पुनरुद्धार आवश्यक है। राजस्थान की कृषि, भले ही अनेक प्राकृतिक बाधाओं का सामना कर रही हो, लेकिन सरकार की योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों और किसानों की मेहनत से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके सतत विकास के लिए जल प्रबंधन, तकनीकी सुधार और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। राजस्थान की कृषि का आर्थिक प्रगति में योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुआयामी है। यह न केवल खाद्य उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिरता, ग्रामीण रोजगार और औद्योगिक विकास को भी प्रभावित करता है। यहाँ की कृषि पर आधारित गतिविधियाँ जैसे पशुपालन, कृषि निर्यात, और कृषि आधारित उद्योग राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान: राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 25-30% के बीच रहता है। यह इंगित करता है कि कृषि न केवल खाद्य उत्पादन का साधन है, बल्कि यह राज्य के आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। 2. रोजगार सृजन में भूमिका: राजस्थान की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े कार्यों में संलग्न है। यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार का प्रमुख स्रोत है और बड़ी संख्या में किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि-आधारित लघु उद्यमों को आजीविका प्रदान करता है। खासकर छोटे और सीमांत किसान अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। 3. पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का योगदान: राजस्थान पशुपालन में अग्रणी राज्य है। यहाँ ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, और भैंस पालन व्यापक रूप से किया जाता है। पशुपालन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि इससे जुड़े उद्योग जैसे डेयरी, ऊन उत्पादन, चमड़ा उद्योग और जैविक खाद उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। • राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। 'अमूल' और 'सरस' जैसी डेयरी सहकारी समितियाँ इस क्षेत्र को संगठित रूप से विकसित करने में सहायक रही हैं। • ऊन उत्पादन: जैसलमेर, बीकानेर, और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में भेड़ पालन से ऊन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो भारत के प्रमुख ऊन उद्योगों में से एक है। 4. कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन: राजस्थान से विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जिससे राज्य को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। प्रमुख निर्यातित उत्पादों में शामिल हैं: • मसाले: जीरा, सौंफ, धनिया और मैथी का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। • जैविक उत्पाद: जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से विदेशी बाजारों में राजस्थान के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है। • बाजरा और सरसों: राजस्थान का बाजरा और सरसों न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। • औषधीय पौधे: अश्वगंधा, एलोवेरा, इसबगोल और अन्य औषधीय फसलें वैश्विक स्तर पर निर्यात की जाती हैं। 5. कृषि आधारित उद्योगों का विकास: राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये उद्योग न केवल कृषि उत्पादों को प्रसंस्करित करने में मदद करते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी सहायक होते हैं। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं: • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: राजस्थान में कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जो गेहूँ, जौ, दालें और अन्य खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण करती हैं। • तेल मिलें: सरसों उत्पादन में अग्रणी होने के कारण, राज्य में कई सरसों तेल मिलें स्थापित हैं, जो स्थानीय किसानों को लाभ प्रदान करती हैं। • डेयरी उद्योग: 'सरस डेयरी' जैसी सहकारी समितियाँ न केवल दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही हैं। • कपास आधारित उद्योग: राज्य में कपास की खेती से जुड़े उद्योग जैसे कपड़ा मिलें, सूती वस्त्र उत्पादन और हस्तशिल्प उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। राजस्थान में कृषि न केवल खाद्य उत्पादन का साधन है, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण घटक भी है। यह न केवल रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, बल्कि पशुपालन, निर्यात और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद, यदि सरकार और किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें, तो कृषि क्षेत्र और भी अधिक आर्थिक समृद्धि ला सकता है। राजस्थान की कृषि से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ राजस्थान में कृषि क्षेत्र कई प्राकृतिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित है, जो इसकी उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन चुनौतियों में जल संकट, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई सुविधाओं की कमी, तकनीकी जागरूकता का अभाव, और बाजार से जुड़ी समस्याएँ प्रमुख हैं। इनका समाधान किए बिना राज्य की कृषि का सतत विकास संभव नहीं है। 1. जल संकट और सिंचाई की चुनौतियाँ: राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु वाला है, जहाँ जल संसाधनों की भारी कमी है। • अनियमित वर्षा: राज्य में औसत वार्षिक वर्षा केवल 100 से 800 मिमी के बीच होती है, जो असमान रूप से वितरित होती है। कई बार लम्बे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। • भूजल स्तर में गिरावट: अत्यधिक जल दोहन और कम वर्षा के कारण राज्य में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। पश्चिमी राजस्थान में कई क्षेत्रों में जलस्तर 100 मीटर से भी अधिक गहराई पर पहुँच चुका है। • सिंचाई सुविधाओं की कमी: राज्य में इंदिरा गांधी नहर, माही बजाज सागर परियोजना और जवाई बांध जैसी कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ हैं, लेकिन ये केवल सीमित क्षेत्रों को कवर कर पाती हैं। अधिकांश किसान अब भी कुओं, ट्यूबवेल और तालाबों पर निर्भर हैं, जो पानी की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन को अस्थिर बनाते हैं। 2. मिट्टी की उर्वरता में गिरावट: लगातार कृषि उत्पादन और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से राजस्थान की मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। • जैविक पदार्थों की कमी: अत्यधिक खेती के कारण मिट्टी में आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और पोटाश की मात्रा कम होती जा रही है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। • रेतीली मिट्टी की समस्या: पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रेतीली मिट्टी अधिक होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है, जिससे फसल उत्पादन में बाधा आती है। • लवणीयता और क्षारीयता: राजस्थान के कई हिस्सों में भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ रही है, जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 3. जलवायु परिवर्तन और कृषि पर प्रभाव: राजस्थान में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे फसलों के बढ़ने और उपज की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। • मानसूनी अनिश्चितताओं के कारण सूखे और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे किसान फसल चक्र को स्थिर रूप से अपनाने में असमर्थ हो रहे हैं। • अत्यधिक गर्मी और जल की कमी के कारण पशुपालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे दूध उत्पादन और पशुओं के चारे की उपलब्धता कम होती जा रही है। 4. तकनीकी जागरूकता और आधुनिक कृषि तकनीकों का अभाव: राजस्थान के अधिकांश किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी से वंचित रहते हैं। • कृषि उपकरणों, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और स्मार्ट फार्मिंग जैसी आधुनिक प्रणालियों को अपनाने में सरकार की योजनाओं का प्रभाव सीमित रहा है। • किसानों को उन्नत बीज, मृदा परीक्षण और जल प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे उत्पादन क्षमता सीमित रहती है। 6. बाजार और मूल्य निर्धारण की समस्याएँ: राजस्थान के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बिचौलियों की संख्या अधिक होने के कारण किसानों को बाजार मूल्य का पूरा लाभ नहीं मिलता। • कई बार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा के बावजूद, किसानों को स्थानीय मंडियों में इससे कम दर पर उपज बेचनी पड़ती है। • भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं की कमी के कारण कई बार किसान जल्दबाजी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 4, April 2025 |
| Published On | 2025-04-22 |
| Cite This | राजस्थान में कृषि का आर्थिक प्रगति में योगदान का भौगोलिक विश्लेषण - Prem Shankar Kirar - IJLRP Volume 6, Issue 4, April 2025. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

