
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 4
April 2025
Indexing Partners
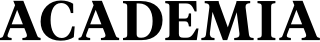




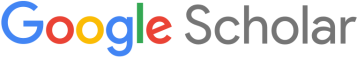













भारत में औपनिवेशिक शासन का सामाजिक प्रभाव ऐतिहासिक अवलोकन
| Author(s) | Pankaj Kumar Shukla |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक कानून बनाए। इन कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, भारतीय समाज को नियंत्रण में रखना और आर्थिक शोषण को सुविधाजनक बनाना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों ने न केवल भारतीय समाज की संरचना को बदला बल्कि सामाजिक वर्गों के बीच संबंधों को भी प्रभावित किया। औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारतीय समाज एक जटिल और विविधतापूर्ण संरचना थी, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, और आर्थिक समूहों का सह-अस्तित्व था। हालाँकि, ब्रिटिश कानूनों ने इस पारंपरिक सामाजिक संरचना में गहरा हस्तक्षेप किया। जहां कुछ कानूनों ने सामाजिक सुधार की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया, वहीं अधिकांश कानूनों का उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक दोहन था। ब्रिटिश सरकार ने कानूनों का उपयोग भारतीय समाज की रीति-रिवाजों, धार्मिक परंपराओं, जातिगत संरचना, तथा स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बदलने में किया, जिससे भारतीय समाज में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश सरकार ने कई सामाजिक सुधार कानून बनाए, जिनमें सती प्रथा निषेध अधिनियम (1829), विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), और बाल विवाह निषेध अधिनियम (1891) प्रमुख थे। इन कानूनों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, किंतु इनके लागू होने के तरीके और उद्देश्यों को लेकर विवाद बना रहा। वहीं, कई ऐसे कानून भी बनाए गए जिन्होंने जाति व्यवस्था को कठोर बना दिया और समाज में कृत्रिम विभाजन को बढ़ावा दिया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ब्रिटिश शासन ने भूमि कर व्यवस्था में परिवर्तन कर किसानों और कारीगरों को भारी करों के बोझ तले दबा दिया। स्थायी बंदोबस्त (1793), रैयतवाड़ी व्यवस्था, और महालवाड़ी व्यवस्था जैसी नीतियों ने भारतीय किसानों को भूमिहीन बना दिया और जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, भारतीय उद्योगों और व्यापार को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी व्यापारिक नीतियाँ लागू कीं, जिससे पारंपरिक कारीगर वर्ग का पतन हुआ और भारत केवल एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनकर रह गया। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में, ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के लिए पृथक कानूनी प्रणाली लागू की। भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) जैसे कानूनों के माध्यम से न्यायिक प्रणाली को औपनिवेशिक शासन के अनुकूल बनाया गया। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) और रॉलेट एक्ट (1919) जैसे कानून लाए गए, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इस शोध पत्र का उद्देश्य औपनिवेशिक काल के प्रमुख कानूनों का विश्लेषण करना और यह समझना है कि इनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि ब्रिटिश कानूनों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार प्रभावित किया और उनके दीर्घकालिक परिणाम क्या रहे। यह शोध पत्र उन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर केंद्रित होगा, जिनका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में देखा गया। ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए कानूनों ने भारतीय समाज की परंपराओं, जातिगत संरचना, धार्मिक रीति-रिवाजों और महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। इन कानूनों का प्रभाव दूरगामी था और स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। औपनिवेशिक शासन की नीति केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। 1. जाति और सामाजिक संरचना पर प्रभाव ब्रिटिश शासन से पहले जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली थी, और सामाजिक गतिशीलता के कुछ अवसर उपलब्ध थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किए गए कानूनों और प्रशासनिक नीतियों ने जातिगत संरचना को कठोर बना दिया। • कानूनी हस्तक्षेप और जनगणना: 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने जातिगत जनगणना (Caste Census) की शुरुआत की, जिससे जातियों का औपचारिक रूप से वर्गीकरण किया गया। यह प्रक्रिया भारतीय समाज के लिए नई थी और इससे जातिगत पहचान और वर्गीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे समाज में जातिगत विभाजन गहरा हुआ। • सामाजिक विभाजन: ब्रिटिश सरकार ने जातियों को उनके पारंपरिक कार्यों तक सीमित करने का प्रयास किया। उन्होंने उच्च जातियों को प्रशासनिक पदों तक सीमित रखा और निम्न जातियों को परंपरागत व्यवसायों तक बनाए रखने की नीति अपनाई। इससे सामाजिक गतिशीलता बाधित हुई और जातिगत भेदभाव मजबूत हुआ। • अछूतों की स्थिति: औपनिवेशिक सरकार ने दलितों (अछूतों) के लिए कुछ सुधारों की पहल की, लेकिन इसने भारतीय समाज में अधिक सामाजिक तनाव उत्पन्न किया। दलितों के लिए आरक्षित विद्यालय और नौकरियों ने उच्च जातियों के साथ उनके संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया। 2. धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ब्रिटिश शासन ने भारतीय धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप किया, जिससे समाज में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। • सती प्रथा निषेध अधिनियम (1829): लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में इस कानून को पारित किया गया, जिसने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। हालांकि, इस कानून को भारतीय समाज के पारंपरिक वर्गों से तीव्र विरोध मिला, क्योंकि इसे ब्रिटिश हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। • विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856): यह कानून हिंदू समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देता था। इसके परिणामस्वरूप समाज के कुछ वर्गों में सुधारवादी आंदोलन को बल मिला, लेकिन रूढ़िवादी वर्गों ने इसे भारतीय परंपराओं पर आघात के रूप में देखा। • धर्म परिवर्तन और मिशनरियों की भूमिका: ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों से भारतीय समाज में धार्मिक संघर्ष और असंतोष बढ़ा। मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से हिंदू और मुस्लिम समाज में अपनी धार्मिक पहचान को बचाने की भावना मजबूत हुई, जिसके परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्य समाज और अन्य हिंदू पुनर्जागरण आंदोलनों की शुरुआत हुई। 3. महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानूनों ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, लेकिन इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध का कारण बनी। • शिक्षा पर प्रभाव: वुड्स डिस्पैच (1854) के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। इससे भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी। 19वीं शताब्दी में पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले और अन्य समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा के लिए सक्रिय योगदान दिया। • बाल विवाह निषेध अधिनियम (1891): इस कानून के तहत लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। यह समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसका कड़ा विरोध भी हुआ। • उत्तराधिकार कानून और संपत्ति अधिकार: ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए कुछ कानून बनाए, जिससे पारिवारिक संरचना प्रभावित हुई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1937) ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान किया, जो पारंपरिक हिंदू परिवार व्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव था। ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों ने भारतीय समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया और कई मामलों में स्थायी परिवर्तन लाए। जाति व्यवस्था की कठोरता, धार्मिक हस्तक्षेप, और महिलाओं की स्थिति में सुधार जैसे मुद्दे भारतीय समाज की संरचना को नए सिरे से परिभाषित करने में सहायक बने। हालाँकि, कई कानूनों के लागू होने से भारतीय समाज में असंतोष भी उत्पन्न हुआ, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। इन औपनिवेशिक कानूनों के प्रभाव आज भी भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में देखे जा सकते हैं। औपनिवेशिक कानूनों का आर्थिक प्रभाव ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए आर्थिक कानूनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों को साधना था, जिससे भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। स्थानीय उद्योगों को हाशिए पर धकेल दिया गया, कृषि को एक नकदी फसल आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया और औद्योगिक उत्पादन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार, औपनिवेशिक आर्थिक कानूनों के कारण भारतीय समाज आर्थिक असमानता, कर्ज, बेरोजगारी और गरीबी की चपेट में आ गया। 1. भूमि संबंधी कानून और किसानों की स्थिति ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों और जमींदारों के संबंधों को पूरी तरह से बदलने वाले कई कानून लागू किए। इन कानूनों ने कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला और किसानों की स्थिति को दयनीय बना दिया। • स्थायी बंदोबस्त, 1793: लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस व्यवस्था ने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया, जिसमें जमींदारों को कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई। इससे किसानों पर करों का बोझ बढ़ा और वे आर्थिक शोषण का शिकार हुए। जो किसान समय पर कर नहीं चुका पाते थे, उनकी भूमि छीन ली जाती थी, जिससे वे भूमिहीन मजदूर बन गए। • रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रणाली: दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत किसानों को सीधे सरकार को कर देना पड़ता था। लेकिन कर की दर इतनी अधिक थी कि किसान भारी कर्ज के जाल में फंस गए। • 1859 का इंडिगो अधिनियम: ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे किसानों का जीवन अत्यधिक कष्टमय हो गया। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्हें दंडित किया गया। यह कानून किसानों की स्थिति सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन इससे उनका आर्थिक शोषण कम नहीं हुआ। • खेती पर अत्यधिक करों का बोझ: ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर करों का भारी बोझ डाला, जिससे वे महाजनों के ऋण पर निर्भर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश किसान अपने पारंपरिक पेशे से हटकर मजदूरी करने को मजबूर हो गए। 2. औद्योगिक और व्यापारिक कानून ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय व्यापार और उद्योगों को कमजोर करने वाले अनेक कानून बनाए गए, जिनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश बाजारों के अनुरूप ढालना था। • भारतीय वस्त्र उद्योग पर प्रभाव: 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ा उद्योग पर भारी कर लगाए और ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों को भारतीय बाजार में बढ़ावा दिया। इस नीति के कारण भारत के बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। उदाहरण के लिए, बंगाल का प्रसिद्ध मलमल उद्योग लगभग समाप्त हो गया। • नौसैनिक कानून और व्यापार नीति: ब्रिटिश नौसैनिक कानूनों के तहत भारतीय जहाजरानी उद्योग को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यापारियों को समुद्री व्यापार से बाहर कर दिया और इस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। • रेलवे और आधुनिक उद्योगों की स्थापना: ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएँ विकसित की गईं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन तक पहुँचाना और ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों को भारतीय बाजार में बेचना था। रेलवे का लाभ आम भारतीय जनता की तुलना में ब्रिटिश व्यापारियों को अधिक मिला। • भारी कर और शुल्क नीतियाँ: ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों पर भारी कर लगाए, जिससे वे धीरे-धीरे अपने व्यवसाय से बाहर हो गए और भारतीय बाजारों में ब्रिटिश उत्पादों का वर्चस्व स्थापित हो गया। 3. आर्थिक असमानता और गरीब वर्ग पर प्रभाव औपनिवेशिक कानूनों ने भारतीय समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। इन नीतियों का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ा— • शहरीकरण और श्रमिक वर्ग: ब्रिटिश औद्योगिक नीति के कारण भारतीय शहरीकरण असंतुलित रूप से विकसित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन वहां भी उन्हें कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था। • महिलाओं पर प्रभाव: पारंपरिक घरेलू उद्योगों के समाप्त होने से महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर होना पड़ा। भारतीय महिलाओं का वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के कारण उनके रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। • भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव: ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो गई। पारंपरिक साहूकारों और स्थानीय बैंकों की जगह ब्रिटिश बैंकों ने ले ली, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्भर हो गई। 4. कृषि अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र में कई बदलाव हुए, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ा— • नकदी फसलों की ओर बदलाव: ब्रिटिश सरकार ने किसानों को गेहूं, चावल, बाजरा जैसी खाद्य फसलों की बजाय नील, अफीम, कपास, जूट और गन्ने जैसी नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया। इससे भारतीय कृषि उत्पादन ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकताओं पर निर्भर हो गया और देश में खाद्य संकट पैदा हुआ। • भुखमरी और अकाल: 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारत में कई भयंकर अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मारे गए। 1876-78 और 1899-1900 के भीषण अकालों में सरकार की निष्क्रियता ने समस्या को और बढ़ा दिया। • महाजनी प्रथा का विस्तार: ब्रिटिश कर नीतियों के कारण किसान कर्ज के जाल में फंस गए और महाजनों व जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाई। ये कानून ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, जबकि भारतीय किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय कृषि व्यवस्था को नकदी फसलों की ओर मोड़ने से देश में खाद्य संकट उत्पन्न हुआ, वहीं पारंपरिक उद्योगों को खत्म करके भारतीय कारीगरों और श्रमिकों को बेरोजगार बना दिया गया। इन नीतियों के कारण भारत एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था बन गया, जो पूरी तरह से ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों पर निर्भर हो गया। इन शोषणकारी नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र कर दिया, जिससे 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। निष्कर्ष ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए औपनिवेशिक कानूनों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इन कानूनों ने न केवल पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक ढांचे को कमजोर किया, बल्कि भारतीय जनता के शोषण को भी संस्थागत रूप दिया। भूमि कर प्रणाली ने किसानों को लगातार ऋणग्रस्त और आर्थिक रूप से असुरक्षित बना दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था लंबे समय तक संकट में रही। व्यापार और औद्योगिक नीतियों ने भारत के स्वदेशी उद्योगों को कमजोर कर दिया, जिससे लाखों कारीगर और मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके अलावा, ब्रिटिश प्रशासनिक और विधायी कानूनों ने भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने के लिए दमनकारी उपायों का सहारा लिया। हालांकि, इन दमनकारी नीतियों और कानूनों के बीच कुछ ऐसे भी कानून थे जिन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की नींव रखी। उदाहरण के लिए, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और शिक्षा से जुड़े सुधार कानूनों ने भारतीय समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाने में योगदान दिया। लेकिन इन सकारात्मक प्रभावों की तुलना में ब्रिटिश कानूनों का कुल प्रभाव भारतीय समाज के आर्थिक और राजनीतिक दमन के रूप में अधिक महसूस किया गया। दीर्घकालिक रूप से, इन औपनिवेशिक कानूनों ने भारतीय समाज में आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलनों को जन्म दिया। सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ बढ़ते आक्रोश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक सशक्त किया। प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध, राजनीतिक अधिकारों के सीमित होने और प्रशासनिक दमन ने राष्ट्रवादी नेताओं और जनता को संगठित होने की प्रेरणा दी। ब्रिटिश शासनकाल के कानूनों का प्रभाव आज भी भारत की प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक संरचना में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने कई औपनिवेशिक कानूनों को संशोधित किया या समाप्त कर दिया, लेकिन कई संस्थागत ढांचे ब्रिटिश काल की देन हैं। इसलिए, इन कानूनों के प्रभाव का अध्ययन न केवल इतिहास की समझ के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद कैसे एक स्वायत्त और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने प्रशासन और नीतियों को विकसित किया। संदर्भ सूची 1. बिपिन चंद्र, भारत में औपनिवेशिक शासन और उसके प्रभाव, पृष्ठ 120-135। 2. रामचंद्र गुहा, भारत का इतिहास: स्वतंत्रता से पहले और बाद में, पृष्ठ 80-95। 3. सुमित सरकार, आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, पृष्ठ 150-170। 4. R.C. Majumdar, British Rule in India, पृष्ठ 200-225। 5. D.N. Dhanagare, Peasant Movements in India, पृष्ठ 50-75। 6. Judith Brown, Modern India: The Origins of an Asian Democracy, पृष्ठ 180-195। 7. Anil Seal, Emergence of Indian Nationalism, पृष्ठ 130-150। 8. Sumit Sarkar, Modern India (1885-1947), पृष्ठ 175-190। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 3, March 2025 |
| Published On | 2025-03-27 |
| Cite This | भारत में औपनिवेशिक शासन का सामाजिक प्रभाव ऐतिहासिक अवलोकन - Pankaj Kumar Shukla - IJLRP Volume 6, Issue 3, March 2025. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

