
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Home
Research Paper
Submit Research Paper
Publication Guidelines
Publication Charges
Upload Documents
Track Status / Pay Fees / Download Publication Certi.
Editors & Reviewers
View All
Join as a Reviewer
Reviewer Referral Program
Get Membership Certificate
Current Issue
Publication Archive
Conference
Contact Us
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 2
February 2025
Indexing Partners
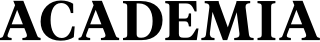




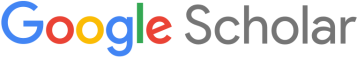













राजस्थान में वन: एक भौगोलिक अध्ययन
| Author(s) | Raghuveer Prasad Suman |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद, वन्य आवरण के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में सीमित संसाधनों वाला क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक विविधता, शुष्क जलवायु और मरुस्थलीय विस्तार वनस्पति संरचना को गहराई से प्रभावित करते हैं। राज्य का अधिकांश भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहाँ वार्षिक वर्षा अत्यंत कम होती है और जलवायु अत्यधिक शुष्क रहती है। इसके बावजूद, राजस्थान में कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जो राज्य की पारिस्थितिकीय समृद्धि को दर्शाती हैं। अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, तथा कुछ मैदानी भागों में वनस्पतियाँ अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई हैं। वन केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि ये राज्य की जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण, तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के वनों में कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर (रणथंभौर और सरिस्का), भारतीय तेंदुआ, चिंकारा, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोदोवन)। इसके अलावा, खेजड़ी का वृक्ष, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में, राजस्थान के वन संसाधनों का उपयोग राजाओं और स्थानीय शासकों द्वारा युद्ध, भवन निर्माण, और विभिन्न हस्तशिल्प उद्योगों के लिए किया जाता रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान वनों का व्यापक दोहन हुआ, जिससे वन आवरण में कमी आई। स्वतंत्रता के बाद, वन संरक्षण को लेकर विभिन्न सरकारी नीतियाँ लागू की गईं, लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण, और औद्योगिकीकरण के कारण आज भी राजस्थान के वनों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह शोध पत्र राजस्थान के वनों की भौगोलिक विशेषताओं, वितरण, महत्व, संरक्षण नीतियों और वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह राज्य में वनीकरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के संभावित उपायों पर भी प्रकाश डालता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण की बढ़ती समस्या को देखते हुए, राजस्थान में वनों का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अनिवार्य विषय बन गया है। 2. राजस्थान के वनों का भौगोलिक वितरण राजस्थान में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.56% (ISFR-2021) है। हालांकि यह प्रतिशत अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन यह राज्य की भौगोलिक विविधता, जलवायु परिस्थितियों और पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुआ है। राजस्थान के वनों का वितरण क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी के प्रकार के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में देखा जाता है। राज्य के वनों को मुख्यतः चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: 1. दक्षिणी अरावली क्षेत्र अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ का वनावरण राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक सघन है। इस क्षेत्र में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, और राजसमंद जिले आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन (Dry Deciduous Forests) पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागवान, खैर, अर्जुन, और शीशम के वृक्ष प्रमुख रूप से मौजूद हैं। यह क्षेत्र वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहाँ रणथंभौर, कुम्भलगढ़, और माउंट आबू जैसे वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। 2. पूर्वी राजस्थान यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं। कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, और बूंदी जिलों में घने जंगलों का विस्तार है। इन वनों में सागवान, शीशम, महुआ, बेर, खैर, और अर्जुन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र भी स्थित हैं, जो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। 3. थार मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहाँ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और नागौर जिले स्थित हैं, अत्यधिक शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक वन बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और अधिकांशतः शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति का प्रभुत्व है। इस क्षेत्र में कैक्टस, खेजड़ी, आक, बेर, और झाड़ीदार वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान के ग्रामीण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मरुस्थलीय परिस्थितियों में भी पनप सकता है और पशुओं के लिए चारा प्रदान करता है। 4. शेखावाटी एवं मध्य राजस्थान झुंझुनू, सीकर, चुरू, अजमेर, जयपुर और दौसा जिलों में कम घनत्व वाले झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा कम होती है, जिससे यहाँ वृक्षों की ऊँचाई भी कम होती है। यहाँ की वनस्पति में बबूल, बेर, खेजड़ी, रोहिड़ा, और नागफनी जैसी झाड़ीदार प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हालांकि यह क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित नहीं है, लेकिन ये झाड़ीदार वन मिट्टी के कटाव को रोकने, कृषि कार्यों में सहायक बनने और स्थानीय जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारक राजस्थान के वनों का वितरण कई भौगोलिक और मानवीय कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें प्रमुख हैं: 1. जलवायु: राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु वाला है, जहाँ वर्षा की मात्रा सीमित होती है। केवल पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ही पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे वहाँ वन अधिक सघन हैं। 2. मिट्टी: पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी और जल की कमी वनों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि अरावली क्षेत्र की मिट्टी वनों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। 3. मानवीय गतिविधियाँ: बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, कृषि विस्तार, तथा अवैध कटाई से राज्य के वन तेजी से प्रभावित हुए हैं। 4. संरक्षण प्रयास: सरकार द्वारा स्थापित वन्यजीव अभयारण्यों, जैव विविधता पार्कों और वृक्षारोपण परियोजनाओं ने कई क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने में योगदान दिया है। राजस्थान के वनों का वितरण मुख्य रूप से जलवायु और स्थलाकृतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। अरावली पर्वतमाला और पूर्वी राजस्थान में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि पश्चिमी और शेखावाटी क्षेत्र में वनस्पति सीमित है। हालाँकि राज्य में वन्य आवरण कम है, फिर भी यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जलवायु नियंत्रण में सहायक बनने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी नीतियों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, जिससे राजस्थान के वन्य संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। 3. वनों का वर्गीकरण राजस्थान के वनों को उनकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिस्थितियों, और वनस्पति संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य का विशाल क्षेत्रफल और विविध स्थलाकृति विभिन्न प्रकार के वनों के विकास में सहायक बनती है। भारत सरकार के भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India - FSI) की रिपोर्ट और पर्यावरणविदों के अध्ययनों के अनुसार, राजस्थान के वनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है: 1. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forests) ये वन राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिक पाए जाते हैं, विशेषकर अरावली पर्वतमाला और हाडौती क्षेत्र (कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, और उदयपुर) में। इन वनों की विशेषता यह है कि शुष्क मौसम में अधिकांश वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे जल की कमी से बचा जा सके। मुख्य वनस्पति: • साल (Shorea robusta) • सागौन (Tectona grandis) • बांस (Bambusa arundinacea) • तेंदू (Diospyros melanoxylon) • महुआ (Madhuca indica) महत्व: • ये वन औषधीय पौधों, लकड़ी, तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। • इन वनों में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, और भालू जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। 2. कांटेदार वनस्पति वन (Thorny Scrub Forests) राजस्थान के पश्चिमी भाग (थार मरुस्थल) और शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कांटेदार झाड़ियों और छोटे वृक्षों से युक्त होते हैं। अत्यधिक शुष्क जलवायु के कारण ये वन बड़े वृक्षों से वंचित रहते हैं, लेकिन इनकी वनस्पति अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती है। मुख्य वनस्पति: • खेजड़ी (Prosopis cineraria) – राजस्थान का राज्य वृक्ष • बबूल (Acacia nilotica) • रोहिड़ा (Tecomella undulata) • बेर (Ziziphus mauritiana) • आक (Calotropis procera) महत्व: • ये वन मरुस्थल के विस्तार को रोकने और स्थानीय पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायक हैं। • पशु चराई के लिए महत्वपूर्ण चारा स्रोत प्रदान करते हैं। 3. नदी तटीय वन (Riparian Forests) ये वन मुख्यतः चंबल, बनास, माही, और कालीसिंध नदियों के तटीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। राजस्थान के इन नदी तटीय क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे यहाँ घनी वनस्पति विकसित होती है। मुख्य वनस्पति: • अर्जुन (Terminalia arjuna) • बड़ (Ficus benghalensis) • पीपल (Ficus religiosa) • जामुन (Syzygium cumini) • सिरस (Albizia lebbeck) महत्व: • ये वन मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। • जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से मगरमच्छ, घड़ियाल, और पक्षियों के लिए आदर्श आवास हैं। 4. सदाबहार वन (Evergreen Forests) राजस्थान में सदाबहार वनों की उपस्थिति बहुत सीमित है, लेकिन दक्षिणी अरावली की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में इनका अस्तित्व पाया जाता है। माउंट आबू क्षेत्र में कुछ मात्रा में ये वन विकसित हुए हैं, जहाँ नमी की अधिकता और अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण वृक्षों की पत्तियाँ पूरे वर्ष हरी रहती हैं। मुख्य वनस्पति: • जंगली अंजीर (Ficus glomerata) • जामुन (Syzygium cumini) • आम (Mangifera indica) • कटहल (Artocarpus heterophyllus) महत्व: • ये वन जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। • जलवायु संतुलन और जल संरक्षण में सहायक होते हैं। वनों के वर्गीकरण का महत्व राजस्थान के वनों का वर्गीकरण उनके संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के वनों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से क्षेत्र वनों की दृष्टि से संवेदनशील हैं और किस क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। • शुष्क पर्णपाती वन वनों की आर्थिक उपयोगिता और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। • कांटेदार वनस्पति वन मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और पशु चारागाह के रूप में कार्य करते हैं। • नदी तटीय वन जल स्रोतों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन में मदद करते हैं। • सदाबहार वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और वन्यजीव संरक्षण में सहायक होते हैं। राजस्थान में वनस्पति आवरण विविधता से भरा हुआ है, जो राज्य की भौगोलिक और जलवायु स्थितियों के अनुसार अलग-अलग प्रकारों में विभाजित है। जहाँ अरावली पर्वतमाला में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वहीं थार मरुस्थल में कांटेदार वनस्पति का वर्चस्व है। इसके अतिरिक्त, नदी तटीय वन और कुछ सीमित सदाबहार वन भी यहाँ की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। इन वनों का सही प्रकार से वर्गीकरण और प्रबंधन न केवल पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। 3. वनों का वर्गीकरण राजस्थान के वनों को उनकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिस्थितियों, और वनस्पति संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य का विशाल क्षेत्रफल और विविध स्थलाकृति विभिन्न प्रकार के वनों के विकास में सहायक बनती है। भारत सरकार के भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India - FSI) की रिपोर्ट और पर्यावरणविदों के अध्ययनों के अनुसार, राजस्थान के वनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है: 1. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forests) ये वन राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिक पाए जाते हैं, विशेषकर अरावली पर्वतमाला और हाडौती क्षेत्र (कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, और उदयपुर) में। इन वनों की विशेषता यह है कि शुष्क मौसम में अधिकांश वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे जल की कमी से बचा जा सके। मुख्य वनस्पति: • साल (Shorea robusta) • सागौन (Tectona grandis) • बांस (Bambusa arundinacea) • तेंदू (Diospyros melanoxylon) • महुआ (Madhuca indica) महत्व: • ये वन औषधीय पौधों, लकड़ी, तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। • इन वनों में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, और भालू जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। 2. कांटेदार वनस्पति वन (Thorny Scrub Forests) राजस्थान के पश्चिमी भाग (थार मरुस्थल) और शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कांटेदार झाड़ियों और छोटे वृक्षों से युक्त होते हैं। अत्यधिक शुष्क जलवायु के कारण ये वन बड़े वृक्षों से वंचित रहते हैं, लेकिन इनकी वनस्पति अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती है। मुख्य वनस्पति: • खेजड़ी (Prosopis cineraria) – राजस्थान का राज्य वृक्ष • बबूल (Acacia nilotica) • रोहिड़ा (Tecomella undulata) • बेर (Ziziphus mauritiana) • आक (Calotropis procera) महत्व: • ये वन मरुस्थल के विस्तार को रोकने और स्थानीय पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायक हैं। • पशु चराई के लिए महत्वपूर्ण चारा स्रोत प्रदान करते हैं। 3. नदी तटीय वन (Riparian Forests) ये वन मुख्यतः चंबल, बनास, माही, और कालीसिंध नदियों के तटीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। राजस्थान के इन नदी तटीय क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे यहाँ घनी वनस्पति विकसित होती है। मुख्य वनस्पति: • अर्जुन (Terminalia arjuna) • बड़ (Ficus benghalensis) • पीपल (Ficus religiosa) • जामुन (Syzygium cumini) • सिरस (Albizia lebbeck) महत्व: • ये वन मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। • जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से मगरमच्छ, घड़ियाल, और पक्षियों के लिए आदर्श आवास हैं। 4. सदाबहार वन (Evergreen Forests) राजस्थान में सदाबहार वनों की उपस्थिति बहुत सीमित है, लेकिन दक्षिणी अरावली की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में इनका अस्तित्व पाया जाता है। माउंट आबू क्षेत्र में कुछ मात्रा में ये वन विकसित हुए हैं, जहाँ नमी की अधिकता और अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण वृक्षों की पत्तियाँ पूरे वर्ष हरी रहती हैं। मुख्य वनस्पति: • जंगली अंजीर (Ficus glomerata) • जामुन (Syzygium cumini) • आम (Mangifera indica) • कटहल (Artocarpus heterophyllus) महत्व: • ये वन जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। • जलवायु संतुलन और जल संरक्षण में सहायक होते हैं। वनों के वर्गीकरण का महत्व राजस्थान के वनों का वर्गीकरण उनके संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के वनों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से क्षेत्र वनों की दृष्टि से संवेदनशील हैं और किस क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। • शुष्क पर्णपाती वन वनों की आर्थिक उपयोगिता और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। • कांटेदार वनस्पति वन मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और पशु चारागाह के रूप में कार्य करते हैं। • नदी तटीय वन जल स्रोतों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन में मदद करते हैं। • सदाबहार वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और वन्यजीव संरक्षण में सहायक होते हैं। राजस्थान में वनस्पति आवरण विविधता से भरा हुआ है, जो राज्य की भौगोलिक और जलवायु स्थितियों के अनुसार अलग-अलग प्रकारों में विभाजित है। जहाँ अरावली पर्वतमाला में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वहीं थार मरुस्थल में कांटेदार वनस्पति का वर्चस्व है। इसके अतिरिक्त, नदी तटीय वन और कुछ सीमित सदाबहार वन भी यहाँ की जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। इन वनों का सही प्रकार से वर्गीकरण और प्रबंधन न केवल पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। 4. राजस्थान के वनों का महत्व राजस्थान में वन निम्नलिखित रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: 1. जलवायु संतुलन – वन वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं और वर्षा को प्रभावित करते हैं। 2. मृदा अपरदन रोकथाम – वनों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होती हैं, विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में। 3. जैव विविधता संरक्षण – रणथंभौर, सरिस्का, और कुम्भलगढ़ जैसे संरक्षित क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, और अन्य वन्यजीवों के लिए वनों का विशेष महत्व है। 4. आर्थिक महत्व – लाख उत्पादन, तेंदू पत्ता, औषधीय पौधे, तथा लकड़ी के उद्योगों के लिए वनों का दोहन किया जाता है। 5. पर्यटन एवं पारिस्थितिकीय योगदान – राजस्थान के वनों में स्थित अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। 5. वनों की स्थिति और संरक्षण चुनौतियाँ राजस्थान में वन क्षेत्र कई कारणों से संकट में है: 1. वन कटाई और अवैध दोहन – औद्योगीकरण, शहरीकरण, और कृषि विस्तार के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। 2. मरुस्थलीकरण – जलवायु परिवर्तन और मानवजनित कारणों से वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। 3. वन्यजीवों के आवास का संकट – तेजी से घटते वन्य क्षेत्र के कारण जैव विविधता खतरे में है। 4. अनुचित कृषि पद्धतियाँ – चराई और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन वनों को नष्ट कर रहा है। 6. वन संरक्षण के प्रयास राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं: 1. अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान – रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, और मरू अभयारण्य जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। 2. वनीकरण अभियान – 'ग्रीन राजस्थान' योजना, वन महोत्सव, और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3. वन अधिनियम एवं नीतियाँ – भारतीय वन अधिनियम, 1927 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। 4. सामुदायिक भागीदारी – जोधपुर में ‘खेजड़ी संरक्षण आंदोलन’ और स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। 7. निष्कर्ष राजस्थान, जो कि मुख्यतः शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु वाला राज्य है, वहाँ वन क्षेत्र सीमित होने के बावजूद पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु संतुलन, और आर्थिक गतिविधियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के वनों का महत्व केवल पर्यावरणीय संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यटन, औषधीय पौधों, कृषि, जल स्रोत संरक्षण, और सांस्कृतिक धरोहरों से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान के प्रमुख वन क्षेत्र जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, रणथंभौर, सरिस्का, कुम्भलगढ़, और माउंट आबू न केवल वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, बल्कि ये पूरे राज्य के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक हैं। हालांकि, राजस्थान में वनों के समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं। निरंतर बढ़ता विकास कार्य, शहरीकरण, औद्योगीकरण, कृषि विस्तार, और अवैध कटाई के कारण वन क्षेत्र में कमी आ रही है। साथ ही, मरुस्थलीकरण (Desertification) और जल संकट भी वनों के लिए एक बड़ी समस्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंधाधुंध खनन से वहाँ के प्राकृतिक वनों को गंभीर नुकसान हुआ है, जिससे भूक्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ और अधिक बढ़ गई हैं। वन संरक्षण की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कानून लागू किए गए हैं, जैसे कि राजस्थान वन नीति, वनीकरण अभियान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम (JFM)। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बिश्नोई समुदाय और अन्य स्थानीय संगठनों द्वारा भी वन संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। वनों के सतत विकास और संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है: 1. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना – विशेषकर मरुस्थलीय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पौधारोपण और वन पुनर्जीवन परियोजनाओं पर ध्यान देना। 2. संवेदनशील वन क्षेत्रों का संरक्षण – अरावली पर्वतमाला और वन्यजीव अभयारण्यों में अवैध खनन और वृक्ष कटाई को रोकना। 3. स्थानीय समुदायों की भागीदारी – वन संरक्षण में बिश्नोई और अन्य पर्यावरण प्रेमी समुदायों की सहभागिता को बढ़ावा देना। 4. टिकाऊ संसाधन प्रबंधन – वन संसाधनों का संतुलित और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनका संरक्षण हो सके। 5. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का सहयोग – प्रभावी नीतियाँ बनाने और वन प्रबंधन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार और नागरिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। 6. पर्यावरण शिक्षा और जन-जागरूकता – आम जनता को वनों के महत्व और संरक्षण के तरीकों के प्रति शिक्षित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, और सामाजिक अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलानी होगी। यदि सही नीतियों और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन को अपनाया जाए, तो राजस्थान के वन क्षेत्र को संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था, जलवायु स्थिरता, और पारिस्थितिकी में भी सकारात्मक योगदान देगा। वन संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य भी है। जब सरकार, स्थानीय समुदाय, वन्यजीव प्रेमी, और आम जनता एकजुट होकर वन संपदा के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, तभी राजस्थान का प्राकृतिक परिदृश्य हरा-भरा और समृद्ध रह सकेगा। संदर्भ सूची 1. भारतीय वन सर्वेक्षण (ISFR-2021) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। 2. राजस्थान वन विभाग (Forest Department of Rajasthan) – राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट। 3. राजस्थान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन नीति 2021 – राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित नीति दस्तावेज। 4. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 – भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण और सतत विकास हेतु जारी नीति। 5. अरावली पर्वत श्रृंखला और वन संरक्षण – राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध पत्रों से संकलित अध्ययन। 6. राजस्थान के जैव विविधता हॉटस्पॉट – भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) द्वारा प्रकाशित अनुसंधान रिपोर्ट। 7. मरुस्थलीकरण और वन पुनर्जीवन रणनीति – संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की रिपोर्ट। 8. स्थानीय समुदायों की भूमिका – बिश्नोई समुदाय के पर्यावरण संरक्षण योगदान पर आधारित विभिन्न शोध पत्र। 9. संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान – भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रकाशित सरकारी दस्तावेज। 10. पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन और वन क्षेत्र – भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट। |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 1, January 2025 |
| Published On | 2025-01-30 |
| Cite This | राजस्थान में वन: एक भौगोलिक अध्ययन - Raghuveer Prasad Suman - IJLRP Volume 6, Issue 1, January 2025. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

