
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Home
Research Paper
Submit Research Paper
Publication Guidelines
Publication Charges
Upload Documents
Track Status / Pay Fees / Download Publication Certi.
Editors & Reviewers
View All
Join as a Reviewer
Reviewer Referral Program
Get Membership Certificate
Current Issue
Publication Archive
Conference
Contact Us
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 2
February 2025
Indexing Partners
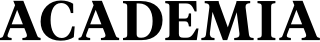




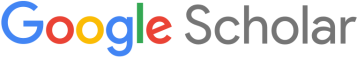













इक्कीसवीं सदी में हिंदी कहानी: स्वरूप, प्रवृत्तियाँ और सामाजिक चेतना
| Author(s) | पप्पू राम |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, क्योंकि इस युग में गद्य साहित्य ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान समय में हिंदी कहानी साहित्यिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरी है, जो विविध सामाजिक विमर्शों को अपने भीतर समेट रही है। आज की कहानियाँ, पूर्ववर्ती कहानियों से कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से अलग हैं। वरिष्ठ साहित्यकारों जैसे संजीव, उदय प्रकाश, ममता कालिया के साथ-साथ चंदन पांडेय, अनिल यादव और पंकज सुबीर जैसे नए दौर के लेखक भी समकालीन समाज की संवेदनाओं को नए मुहावरों और शैलियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में, इन रचनाओं का गहन मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। यह आलेख इक्कीसवीं सदी में हिंदी कहानियों के बदलते स्वरूप को रेखांकित करता है। हिंदी कहानी, अपने प्रारंभिक दिनों से ही साहित्य के सामाजिक सरोकारों को प्रखरता से व्यक्त करती आई है। मानव जीवन के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को अपनी विधागत स्पष्टता और प्रभावशीलता के कारण कहानी ने न केवल एक समृद्ध परंपरा का निर्माण किया है, बल्कि यह भी प्रमाणित किया है कि जीवन के तमाम विमर्शों को वह सशक्त रूप से उजागर कर सकती है। यही कारण है कि दलित, आदिवासी और स्त्री अस्मिता जैसे विमर्श कहानियों में न केवल स्थान पा रहे हैं, बल्कि अपने विचारों को मुखरता से प्रस्तुत करते हुए नए सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आज हम इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में जी रहे हैं, और भारत की आजादी के चौहत्तर वर्ष पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके, कई समस्याएँ और ज्वलंत प्रश्न आज भी हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। जातिवाद, स्त्री-शोषण और किसानों की समस्याएँ तो पहले से ही समाज का हिस्सा थीं, लेकिन भूमंडलीकरण के इस दौर में कई नई और जटिल समस्याएँ उभरी हैं। इनमें आदिवासियों का विस्थापन, संस्कृति का बाजारीकरण, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था का विस्तार, सूचना-तकनीक का जाल, और इसके माध्यम से युवाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण जैसी समस्याएँ शामिल हैं। समकालीन हिंदी कहानी ने इन नए सामाजिक मुद्दों को न केवल स्थान दिया है, बल्कि इन्हें मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर उभारते हुए पाठकों को झकझोरने और उन्हें समाधान की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास भी किया है। इक्कीसवीं सदी के हिंदी कहानीकारों ने जटिल होते मानवीय संबंधों, प्रेम जैसे संवेदनशील मनोभावों पर बाजार के प्रभाव, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मानी जाने वाली मीडिया के नैतिक पतन, युवाओं में दिखावे की प्रवृत्ति, और यौन कुंठा जैसे विषयों को अपने लेखन का हिस्सा बनाया है। 'हंस' पत्रिका के अगस्त 2005 के अंक में छपी उदय प्रकाश की 'मोहनदास' कहानी इन परिवर्तनों के उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। 'मोहनदास' एक ऐसे दलित युवक की कहानी है जिसके नाम और पहचान की डकैती कर ली गई है और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर 'कोल्माइन्स' में नौकरी कर रहा है। उदय प्रकाश ने इस कहानी में भूमंडलीकरण एवं सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग कथ्य एवं शिल्प दोनों स्तरों पर किया है। चलती कहानी के दौरान कहानीकार कई बार पाठक को रोकते हुए चलता है और पाठक को वर्तमान स्थितियों से जोड़ता है। कहानी में कल्पना एवं यथार्थ का मिश्रण है लेकिन पाठक को रोकने के बाद जो संवाद करता है वह विशुद्ध यथार्थ है। जैसे कहानीकार कहता है कि "जो ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत है, वह उसी समय का है जब 9-11 सितम्बर हो चुका है और न्यूयार्क की दो गगनचुम्बी इमारतों के गिरने कि प्रतिक्रिया में एशिया के दो सार्वभौमिक संप्रभुता-संपन्न राष्ट्रों को मलवे में बदला जा चुका है।" इन कहानियों ने न केवल कथ्य के स्तर पर बल्कि शिल्प के स्तर पर भी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों से अलग पहचान बनाई है। वर्तमान सदी के पहले दशक से ही इन कहानियों में एक नया दृष्टिकोण और सामाजिक परिप्रेक्ष्य उभरता दिखाई देने लगता है। ये कहानियाँ न केवल समाज की समस्याओं का दस्तावेज़ बनती हैं, बल्कि पाठकों को उन समस्याओं के प्रति जागरूक करने और समाधान की दिशा में सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इस तरह के प्रयोग से कथ्य के स्तर पर यह कहानी एक वेरोजगार और व्यवस्था के द्वारा छला गया युवक मोहनदास की कहानी मात्र नहीं रहकर पाठक को वैश्विक स्तर की भी महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ती है, दूसरी बात यह कि इस तरह के शिल्प का प्रयोग उदय प्रकाश सीधे सूचना प्रोद्योगिकी के जबरदस्त माध्यम टेलीविजन से सीधे उठा कर कहानी में ले आये हैं। उदय प्रकाश कहते हैं कि एक ओर जहाँ "जो लोग सत्ता में हैं, उसमें से हर कोई एक दूसरे का क्लोन है। हर कोई एक जैसी ब्रांड का उपभोक्ता है। वह एक जैसी चीजें पी रहा है, एक जैसी चीजें खा रहा है। एक जैसी कंपनियों के कार में घूम रहा है। "2 वहीं दूसरी ओर मोहनदास और उसका परिवार जीवन-मौत से संघर्ष कर रहा है। आज राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, झूठ और फरेब का बोलवाला है। अखिलेश की कहानी 'शृंखला' में रतन नामक पात्र की एक ऐसी ही कहानी है। पेशे से प्रोफेसर रतन आँखों से अंधा रहता है। 'जनादेश' अखवार के संपादक महोदय के विशेष प्रार्थना पर 'अप्रिय' नामक कॉलम लिखता है। 'अप्रिय' कॉलम की पहली ही किस्त में रतन लिखता है "शब्दों के शार्ट फार्म (लघु रूप) दरअसल सत्य को छुपाने और उसे वर्चस्वशाली लोगों तक सीमित रखने के उपाय होते हैं। अगर तुम सत्ता से लड़ना चाहते हो तो उसकी प्रभुत्व-संपन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को उनके पूरे नाम से पुकारो।"3 रतन अपने मत को स्पष्ट करने के लिए 'जनादेश' के एक कॉलम में लिखते हैं कि "किसी राजनीतिक दल का पूरा नाम एक प्रकार से उसका मुख़्तसर घोषणा-पत्र होता है। उनके नाम के मूल और समग्र रूप में उनका इतिहास, उनके विचार-सरोकार और जनता को दिखाए गए सपने शामिल रहते हैं। उसने अपने मत को स्पष्ट करने के लिए माकपा का जिक्र किया था। उसने लिखा था - माकपा का मूल नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) है। इस संज्ञा से पता चलता है कि इसका निर्माण कम्युनिज्म, मार्क्सवाद, क्रान्ति और सामाजिक परिवर्तन के सरोकारों के तहत हुआ था। आप सभी को मालूम है कि तमाम पार्टियों की तरह यह पार्टी भी आज इन सब पर कायम नहीं है इसलिए 'माकपा' उसके लिए एक रक्षा कवच है। यह संबोधन अपने उद्देश्यों से इस पार्टी की फिसलन को हँकता है और ऐसे भ्रम की रचना करता है कि साम्यवाद और सर्वहारा कभी इसकी बुनियादी प्रतिज्ञा थे ही नहीं। यही बात अपने नाम का संक्षिप्तीकरण करने वाले अन्य राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है।" रतन कुमार के इस कॉलम के वाद उस पर कातिलाना हमला होता है। अंधे होने के कारण रतन कुमार सबूत नहीं जुटा पाता है जिससे अपराधी बार-बार वच निकलता है। रतन कुमार व्यवस्था के प्रति खूब गुस्सा जाहिर करता है। यह गुस्सा रतन कुमार के रूप में अखिलेश का गुस्सा है। रतन कुमार कहता है "साथियों, सबूत की इस लाठी से राज्य ने हर गरीब, प्रताड़ित और दुखियारे को मारा है। आज इस देश में असंख्य ऐसे परिवार हैं जो अन्न, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित हैं किन्तु राज्य इनकी पुकार सुनने की जरुरत नहीं महसूस करता है। क्योंकि इन परिवारों के पास अपनी यातना को सिद्ध करने वाले सबूत नहीं हैं। हत्या, वलात्कार, भ्रष्टाचार के अनगिनत मुजरिम गुलछर्रे उड़ाते हैं क्योंकि उनके अपराध को साबित करने वाले सबूत नहीं हैं। पुलिस, सेना जैसी राज्य की शक्तियाँ जनता पर जुल्म ढाती है तथा लोगों का दमन, उत्पीड़न, वध, बलात्कार करके उन्हें नक्सलवादी, आतंकवादी बता देती है और कुछ नहीं घटता है। क्योंकि सबूत नहीं है। इस सबूत के चलते देश के आदिवासियों से उनकी जमीन, जंगल और छीन लिए गए क्योंकि आदिवासियों के पास अपना हक साबित करने वाले सबूत नहीं हैं। न जाने कितने लोग अपने होने को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनके पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड नहीं है। दरअसल इस देश में सबूत ऐसा फंदा है जिससे मामूली और मासूम इंसान की गर्दन कसी जाती है और ताकतवर के कुकृत्यों की गठरी को परदे से ढँका जाता है। 5 रतन कुमार कहता है कि "मेरी टूटी हुई हड्डियाँ देखिये। ये मेरी हड्डियाँ नहीं टूटी हैं, इस देश के लोकतंत्र को फ्रेक्चर हो गया है। मेरा अपाहिजपन दरअसल इस देश के शक्तिपीठों की क्रूरता औरन्याय प्रणाली की विकलांगता को दर्शाता है। इस कहानी का अंत एक कल्पना से होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि देश में लोग सरकार, धनिकों और धर्माधीशों के खिलाफ सड़क पर उतर आये हैं और सचमुच में क्रान्ति होने वाली है। अखिलेश इस कहानी में राज्य-सत्ता की आलोचना करते हैं। अजय तिवारी जी के अनुसार "कभी समाजवाद के सपने के साथ नए इंसान की ऐसी सांस्कृतिक कल्पना पेश की गई थी। आख्यान के रूप में उसी सपने को इक्कीसवीं सदी के अनुरूप ढालकर अखिलेश हिंदी के समकालीन रचनाकारों के आगे एक विकल्प प्रस्तावित करते हैं।"" बीते हुए कल के निर्णयों का प्रभाव आने वाले कल की स्थितियों में अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में, जब भारत ने मुक्त व्यापार और उदारीकरण की राह अपनाई, तो समाज और संस्कृति पर बाजार का प्रभाव तेजी से स्पष्ट होने लगा। इस प्रभाव को पंकज सुबीर ने अपनी कहानी 'सदी का महानायक उर्फ़ कूल-कूल तेल का सेल्समेन' (हंस, दिसंबर 2010) में अत्यंत गहनता और सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है। कहानी बाजारवाद के बढ़ते दायरे को उजागर करते हुए यह दिखाती है कि कैसे बाजार ने प्रेम, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं को अपने अधीन कर लिया है। पंकज सुबीर अपनी रचना में बाजार की चालाकी और उसके विस्तृत प्रभाव को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, "बाजार ने धीरे-धीरे उन सारी कहावतों और मुहावरों के अर्थ सीख लिए हैं जो प्यार, प्रेम और मुहब्बत से जुड़ी हुई कहावतें हैं। तभी तो बाजार धीरे-धीरे उन सभी रिश्तों में समा गया है, जिनके भीतर यह तथाकथित प्रेम, प्यार और मुहब्बत मौजूद है।" यह दिखाता है कि बाजार ने हमारे संबंधों को किस प्रकार वस्तुवादी बना दिया है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उसके लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता है, तो बाजार तुरंत हस्तक्षेप करता है और कहता है, "तारों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, यह देखो हमारा लेटेस्ट मोबाइल। तीस हजार का है और आज के समय में यह किसी आसमान के तारे से कम नहीं है। इसे खरीदो और उसे दे दो। उसके लिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा।" यह संवाद इस बात का सटीक उदाहरण है कि बाजार ने किस हद तक हमारी सोच, भावनाओं और रिश्तों को प्रभावित किया है। बाजार आज यह तय करता है कि हम क्या खाएँ, क्या पहनें, कहाँ जाएँ और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों के प्रति अपने भाव कैसे व्यक्त करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दैत्याकार स्वरूप ने मानो हमारी स्वतंत्रता को इस कदर सीमित कर दिया है कि हम अपनी पसंद और इच्छाओं के स्थान पर बाजार के निर्देशों का पालन करने को बाध्य हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं, जहाँ ग़ालिब की मशहूर पंक्तियाँ भी अपना अर्थ खो बैठती हैं: "दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीददार नहीं हूँ।" अब यह स्थिति बदल चुकी है। बाजार ने हमें इस प्रकार घेर लिया है कि ग़ालिब की इस विचारधारा को अपनाना लगभग असंभव हो गया है। बाजार ने न केवल हमारे भौतिक जीवन को नियंत्रित किया है, बल्कि हमारी भावनात्मक और सांस्कृतिक जड़ों को भी गहराई से प्रभावित किया है। पंकज सुबीर की यह कहानी इस विडंबना को बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है, जिससे आज का पाठक अपने समय और समाज के सत्य से रूबरू होता है। 'सदी का महानायक उर्फ़ कूल-कूल तेल का सेल्समेन' कहानी का पात्र शाहरुख अपने दोस्त धोनी के कहने पर अपनी प्रेमिका शिल्पा (जिसपर पहले से बाजार का भूत चढ़ चुका है) को इम्प्रेश करने के लिए बाजार की शरण में जाता है। कहानीकार पंकज सुबीर ने यहाँ शाहरुख और धोनी के बीच हुए वार्तालाप के द्वारा अच्छा संकेत किया है- "ये कौन-सी चड्डी पहनते हो तुम?" ऐन दूकान के सामने धोनी ने रोककर मुझसे पूछा। "चड्डी...?" मैंने अकचकाकर मैंने प्रतिप्रश्न किया। "कच्छा, चड्डी, अंडरवियर और पर्यायवाची गिनवाऊँ कि बस ?" कुछ झुंझलाकर उत्तर दिया था उसने। वही पहनता हूँ जो पहनना चाहिए पर तुमको इससे क्या? और तुमने कब देखी मेरी चड्डी?" मैंने गुस्से में कहा। "अभी जब तुम झुककर जूते की लेस ठीक कर रहे थे, तब तुम्हारी शर्ट ऊपर हो जाने के कारण तुम्हारी पैंट में से देखा था तुम्हारी चड्डी का ब्रांड। शर्म नहीं आती?" धोनी ने कहा। "क्यों भाई शर्म क्यों आएगी। शर्म तो तब आये जब मैं बिना पैंट के केवल कच्छे में घूम रहा हूँ।" मैंने उत्तर दिया।" कच्छे में घूमना कोई शर्म की बात नहीं है, बस कच्छा ब्रांडेड होना चाहिए। और अगर कच्छे में न भी घूम पाओ तो कम से कम पैंट को इतना नीचे खिसकाकर पहनो कि तुम्हारी चड्डी का ब्रांड दिखाई दे। ये केवल चड्डी नहीं है, ये तुम्हारा स्टेटस है, समझे?" धोनी ने कुछ डाँटने वाले लहजे में कहा"10 शाहरुख तो इसमें प्रतीक के रूप में है, वास्तव में हम सब धीरे-धीरे इसके शिकार हो रहे हैं। कहानी के अंत में दिखाया गया है कि सदी का महानायक अपने बेटे, बहु और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ग्राहकों को सामान खरीदवाने में लगा हुआ है यानि विज्ञापन कर रहे हैं। पंकर सुवीर बताते हैं कि हम लाचार हैं, वेवस हैं और बाजार लगातार हमें रौंदता ही जा रहा है। वर्तमान समय की विसंगति की अभिव्यक्ति हिंदी कहानियों में जोरदार ढंग से हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व कहा था- 'खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीद्दमान, सोच-वस, कहैं एक एकं सों' कहाँ जाई, का करी?"11 आज भी समाज में ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना किया जा रहा है, जहाँ मानवीय संवेदनाएँ और सामाजिक असमानता अपनी पराकाष्ठा पर हैं। 'हंस' पत्रिका के दिसंबर 2011 के अंक में प्रकाशित विनय कुमार पटेल की कहानी 'मजबूरन' इसी प्रकार के यथार्थ को उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसे समाज का कड़वा सच प्रस्तुत करती है, जहाँ इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी लोग भूख के कारण अपनी अस्मिता और मानवीय मूल्यों से समझौता करने को मजबूर हैं। कहानी की मुख्य पात्र टेरेसा खाल्को, जो चाय बगान में मजदूरी करती है, अपने पति की असमय मृत्यु और बगान बंद हो जाने के कारण ऐसी परिस्थितियों में घिर जाती है कि उसे अपनी सात वर्षीय बेटी को बेचने का कठोर निर्णय लेना पड़ता है। बच्ची का खरीदार पकड़ा जाता है, लेकिन टेरेसा को पुलिस स्टेशन में टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद, वह अपनी बच्ची को जहर देकर खुद भी आत्महत्या कर लेती है। इस दर्दनाक घटना की खबर अखबार के पहले पृष्ठ पर जगह नहीं पाती; वहाँ एक अभिनेत्री की चमकती तस्वीर और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के 2020 तक के दावे छाए रहते हैं। वित्तमंत्री सेंसेक्स के 18,000 का आंकड़ा पार करने पर गर्वित हैं और भारत के आर्थिक प्रगति के दावे किए जा रहे हैं। इस कहानी में भूख से त्रस्त समाज की दयनीय स्थिति के साथ-साथ मीडिया की संवेदनहीनता को भी तीखे ढंग से उजागर किया गया है। इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानियों ने इसी तरह की गहरी सामाजिक विडंबनाओं को अपने कथ्य और शिल्प में स्थान दिया है। वंदना राग की कहानी 'आज रंग है', विमलचंद्र पांडेय की 'पवित्र सिर्फ एक शब्द है', उमाशंकर चौधरी की 'मिसेज वाटसन की भुतहा कोठी', श्रीकांत दुबे की 'गुरुत्वाकर्षण', चंदन पांडेय की 'मुहर' और 'जमीन अपनी तो थी', कुनाल सिंह की 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जैसी कहानियाँ समकालीन संवेदनाओं और शिल्प के नए तेवर प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों में समाज के विभिन्न आयामों, जटिल होते मानवीय संबंधों, वर्ग-संघर्ष, स्त्री-विमर्श, और बाजारवाद की काली छाया को नए अंदाज़ में व्यक्त किया गया है। यह कहानियाँ न केवल पाठकों को झकझोरती हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रेरित भी करती हैं। इन रचनाओं में कथ्य और शिल्प का यह नवाचार समकालीन हिंदी कहानी को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संदर्भ सूची 1. उदय प्रकाश, मोहनदास, पृष्ठ संख्या-29 2. वही 3. शृंखला-अखिलेश, नया ज्ञानोदय, मई 2011, पृष्ठ संख्या-16 4. वही पृष्ठ संख्या-19 5. वही पृष्ठ संख्या-30 6. सत्ता की क्रूर कथा-अजय तिवारी, नया ज्ञानोदय, मई 2011, पृष्ठ संख्या-38 7. 'सदी का महानायक उर्फ़ कूल-कूल तेल का सेल्समेन-पंकज सुबीर, 'हंस', दिसंबर 2010, पृष्ठ संख्या-21 8. वैश्वीकरण, विज्ञान और वाजार की राजनीति-जीतेन्द्र भाटिया, आलोचना, (उधृत) जनवरी-मार्च 2001, पृष्ठ संख्या -152 9. 'सदी का महानायक उर्फ़ कूल-कूल तेल का सेल्समेन-पंकज सुबीर, 'हंस', दिसंबर 2010, पृष्ठ संख्या-21 10. कवितावली गोस्वामी तुलसीदास लोकभारती प्रकाशन, दिल्ली वर्ष-2009, पृष्ठ संख्या-151 11. मजबूरन-विनय कुमार पटेल, 'हंस', दिसंबर 2011, पृष्ठ संख्या-49 |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 1, January 2025 |
| Published On | 2025-01-27 |
| Cite This | इक्कीसवीं सदी में हिंदी कहानी: स्वरूप, प्रवृत्तियाँ और सामाजिक चेतना - पप्पू राम - IJLRP Volume 6, Issue 1, January 2025. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

