
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Home
Research Paper
Submit Research Paper
Publication Guidelines
Publication Charges
Upload Documents
Track Status / Pay Fees / Download Publication Certi.
Editors & Reviewers
View All
Join as a Reviewer
Reviewer Referral Program
Get Membership Certificate
Current Issue
Publication Archive
Conference
Contact Us
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 2
February 2025
Indexing Partners
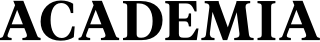




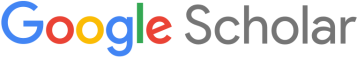













इन्द्रधनुष के रंगों में बसी प्रेम कहानी
| Author(s) | जगदीश |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | प्रेम एक संवेग ही नहीं, बल्कि एक स्थायी भाव भी है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामूहिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक व्यापक होता है। प्रेम की महिमा इसके मानसिक और भावनात्मक स्थायित्व में निहित है, जो इसे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होने की क्षमता प्रदान करता है। यह न केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि संकुचित व्यक्तिगत भावनाओं से लेकर व्यापक वैश्विक स्तर तक इसके अनेक रूप दिखाई देते हैं। कभी यह आत्मप्रेम के रूप में, कभी दाम्पत्य प्रेम के रूप में, और कभी यह कुटुम्ब प्रेम के रूप में मनोवैज्ञानिक स्थायी भाव का रूप धारण करता है। श्रीनरेश मेहता के उपन्यास 'प्रथम फाल्गुन' में महिम और गोपा के प्रेम संबंधों के माध्यम से उपन्यासकार ने स्त्री-पुरुष के मनोभावों और समाज के दबावों का जीवंत चित्रण किया है। महिम अपने प्रेम को प्रकट करता है, जबकि गोपा अपने मनोभावों और पीड़ा को अपने भीतर समेटने का प्रयास करती है। इस उपन्यास में समाज की संरचना इस तरह से प्रस्तुत की गई है कि यह व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी गहरे प्रभाव डालता है, चाहे वह निर्णय कितना भी व्यक्तिगत क्यों न हो। प्रेम का संबंध 'जानने' (ज्ञान) और 'होने' (अस्तित्व) के द्वंद्व से जुड़ा हुआ है, और इसे हम द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से ही समझ सकते हैं। मनुष्य की चेतना उसके कर्मों को निर्देशित करती है, लेकिन चेतना का जन्म कर्म और मनोभाव से होता है। इस प्रकार चेतना और कर्म के बीच निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। ये दोनों कभी अलग होते हैं, कभी संघर्ष करते हैं, और अंततः एक दूसरे में मिलकर निरंतर विकसित होते रहते हैं। बीज शब्दः- प्रेम, समाज, मूल्यबोध, द्वन्द्व, मूल्यों का टकराव, आधुनिकता, भावना, संवेदना । मूल आलेख:- "तुम यहाँ बैठी थीं अभी उस दिन सेब-सी बन लाल चिकने चीड़ सी वह गाँठ अपनी टेक पृथ्वी यहाँ इस पेड़ जड़ पर बैठ/मेरी राह में इस धूप में बह गया वह नीर/जिसको पदों से तुमने छुआ था।" श्रीनरेश मेहता ने स्मृति के द्वारा इस कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति की है, किन्तु वियोग व्यथा को कितने सांकेतिक रूप में अंकित किया है- "चाहता मन तुम यहाँ बैठी रहो उड़ता रहे चिड़ियों सरीखा वह तुम्हारा श्वेत आँचल किन्तु अब तो ग्रीष्म तुम भी दूर और यह लू।" अपनी प्रेयसी की सुन्दरता को कवि प्रकृति के सर्वविदित बिम्बों द्वारा अभिव्यंजित करता है। नरेश मेहता कविता की रूमानियत में स्वच्छन्द होकर कहते नहीं, वह आत्म-विवेक तथा भारतीय-तत्त्व दर्शन से उसे काव्यानुभूति के नए धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं, स्नेह है तो विरह होगा ही।' प्रेम मानव चेतना का आदर्श स्तर है। प्रेम को विभिन्न रूपों में जाना जाता है, जैसे स्त्री-पुरुष के लैंगिक सम्बन्ध के रूप में, पुरुष-पुरुष की मित्रता के रूप में, माता-पिता और सन्तान के बीच या परिवार के अन्य लोगों के बीच वात्सल्य और स्नेह के सम्बन्ध के रूप में। इन तमाम सम्बन्धों को प्रेम का ही नाम दिया जाता है। यह आकस्मिक नहीं है कि लोगों के मन और जीवन को प्रेरित करने वाले सभी महान धर्मों में प्रेम पर इतना जोर दिया गया है। धर्म जब ईश्वर, मोक्ष, स्वर्ग आदि की कल्पनाओं के बारे में बात करता है, तो वह दरअसल प्रेम की बात ही कर रहा होता है, क्योंकि वह समस्त सामाजिक सम्वन्धों को प्रेम के माध्यम से ही सम्भव मानता है। प्रेम के रूप में सामाजिक सम्बन्ध ही मनुष्य के अवचेतन में रहते हैं और धर्म उन्हीं सम्बन्धों को प्रतीकात्मक रूप देकर अपना मूल्य प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रेम है या प्रेम ही ईश्वर है। सामाजिक सम्बन्धों में कोमलता वहाँ होती है, जहाँ मनुष्य दूसरे मनुष्यों को भी मनुष्य मानता है और उनकी मनुष्यता का आदर करता है। यह आदर एक व्यक्ति द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है और उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण दिया जाता है, इसलिए इसमें व्यक्तित्व की पहचान और उसका मान करना शामिल है। ऊपरी तौर पर व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में व्यक्ति समाज को उसकी आन्तरिक चालक शक्ति प्रदान करता है और समाज अपने आन्तरिक विकास से अपनी इकाइयों को व्यक्तित्ववान बनाता है। अतः व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध यांत्रिक मात्र नहीं होते बल्कि उनमें वह भावनात्मक तत्त्व भी होता है जो मानवीय जीवन को जिजीविषा प्रदान करता है। इसी प्रक्रिया में मानवीय बोध का निर्माण होता है, जो व्यक्तित्व को जन्म देता है और व्यक्तित्व से यह चेतना पैदा होती है जिसके कारण सामाजिक उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों में एक तनाव जन्म लेता है। यह तनाव भौतिक या शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक या भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति को महसूस होता है और उसे लगता है कि उसका जीवन क्रूर और कठोर होता जा रहा है। अतः वह उत्पादन के सम्बन्धों में (जो आर्थिक ही नहीं, सामाजिक सम्बन्ध भी होते हैं) सचेत रूप से कोमलता उत्पन्न करने का प्रयास करता है और यह प्रयास प्रेम को जन्म देता है। इस सन्दर्भ में श्रीनरेश मेहता द्वारा लिखित उपन्यास 'प्रथम फाल्गुन' का अध्ययन किया जा सकता है। इस उपन्यास में लेखक ने गोपा और महिम के प्रेम सम्बन्धों का चित्रण किया है। 'प्रथम फाल्गुन' उपन्यास में सांस्कृतिक बोध की दृष्टि से उपन्यासकार ने भारतीय संस्कृति पर पड़े पाश्चात्य संस्कृति के अपरिहार्य प्रभाव की गहराई को संकेतित किया है। साथ ही, आभिजात संस्कृति एवं नूतन भारतीय संस्कृति के विविध आयामों को भी प्रसंगानुकूल उद्घाटित किया है। इस उपन्यास का कथानक उस प्रथम प्रेम की मार्मिकता को अभिव्यक्त करता है, जिसका सम्मोहन सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक होता है। उपन्यास में दो पात्र हैं- गोपा और महिम। आज से तीस-चालीस वर्ष पहले का लखनऊ। परिपाश्र्व की इस ऐकान्तिकता के साथ-साथ दो पात्रों का अपना निजीपन, जहाँ तीसरे का कोई अर्थ या महत्त्व नहीं। रागात्मकता के किन-किन और कैसे-कैसे प्रसंगों, स्थितियों तथा मुद्राओं से होकर गोपा और महिम यात्रा करते हैं यह इस उपन्यास की बुनावट, भाषा तथा प्रतीकों के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रभाकर श्रोत्रिय के अनुसार "स्वातत्र्योत्तर भारतीय समाज में व्यक्ति स्वात्र्य की चेतना से प्रेम-सम्बन्धों में तीव्रता से बदलाव आया है। प्रेम भावुकतापूर्ण एवं सौन्दर्याश्रित न रहकर नितान्त व्यक्तिगत अनुभव की वस्तु बन गया है। प्रेम सम्बन्धों के कई कोण उजागर होते हैं। नयी चेतना की जागृति के कारण स्त्री और पुरुष समान अहं वाले हैं तथा उनका व्यक्तित्व भी समान है, इस कारण प्रेम सम्बन्धों में अपने अस्तित्व का संघर्ष एवं बचाव दोनों दिखाई देते हैं। समग्र परिवेश के नैतिक मान-मूल्यों में इतना बदलाव आ गया है कि प्रेम श्लील-अश्लील, पाप-पुण्य की धारणाओं में परिवर्तित हो गया है।"। लेखक का मानना है कि प्रेम के मामलों में वास्तव में हम अभी तक मध्ययुगीन, नाटकीयतापूर्ण स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाये हैं। कहते भले ही रहें कि नहीं, हम खूब सोच-समझकर आचार-व्यवहार कर रहे हैं, पर वस्तुतः हम भावावेश में होते हैं, शायद प्रेम की स्थिति में यथार्थता का बोध सम्भव ही नहीं हुआ करता। यथार्थ कटु होता है, जबकि प्रेम, धूप में हिलते इन्द्रधनुष का भ्रम देता है। जो भी प्रेम के इस भ्रम को तोड़ता है, वह संकटपूर्ण स्थिति पैदा करता है। ऐसी ही स्थिति महिम के साथ उपस्थित होती है जब उसे गोपा के जारज होने का पता लगता है। यद्यपि महिम गोपा को बहुत प्यार करता है, वह एक स्थान पर गोपा से कहता है:- "अब केवल इतना ही सच है कि गोपा! अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता... पता नहीं, इतनी सीधी-सी बात की अभिव्यक्ति तुम्हारे निकट कुछ होती भी है कि नहीं। जबकि मैं स्पष्टतः यह कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे पाश्र्व में खड़ी हो जाओ।"2 एक अन्य स्थान पर वह गोपा से कहता है:- "गोपा! मैं तुम्हें आकण्ठसज्जित देखना चाहता हूँ... जैसे कदम्ब होता है न, बस वैसे ही... लेकिन नहीं... मैं तुम्हें उस रूप में या उतना सज्जित नहीं देख सकता... मैं तुम्हें तुम्हारे नैसर्गिक रूप से देखना चाहता हूँ... मेरा मतलब तुम जिस तरह अपने को देखती होगी न बस... वैसे ही.... मेरा मतलब यह गोपा! कि तुम्हारे और अपने बीच मैं अब न कोई परिधान, व्यक्ति, तर्क, संशय कुछ भी नहीं चाहता... केवल तुम और मैं... हाँ बस, लेट देम सी अस टुगेदर।"3 इसके बाद भी महिम और गोपा का सम्बन्ध सामान्य नही हैं, क्योंकि गोपा एक जारज सन्तान थी और यह बात महिम को सोचने को बाध्य करती है। निम्नलिखित पंक्तियाँ भी इसी को पुष्ट करती हैं- "हमारे जीवन का नितान्त गोपनीय पक्ष भी समाज-सापेक्ष ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समाज का एक ऐसा सदस्य छुपा बैठा रहता है, जो हमारी सारी व्यक्तिगतता को नियंत्रित करता चलता है। "4 उपन्यास में नायक महिम को जब यह पता चलता है कि गोपा नाथ बाबू की पुत्री नहीं है तो उसके मन में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं, क्योंकि वह गोपा से प्रेम करता है, वहः यह जानकर समाज उसके बारे में क्या सोचेगा? इसी बात के डर से महिम की सारी उत्कंठा, सारा गम्भीरत्व, सारा प्रेम और सारी संवेदनशीलता हार जाती है। लेखक ने महिम के मानसिक द्वन्द्व का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है। यथा "गोपा नाथ बाबू की पुत्री नहीं है, तो क्या? लेकिन इस तर्क से वह अपने अवचेतन तक में कोई समाधान, निष्कर्ष ऐसा खोज नहीं पा रहा था, जिसके कारण वह आश्वस्त हो सकता। उसे लगा जैसे वह अभी तक किसी प्राचीन इमारत की बड़ी सी दीवार के सहारे खड़ा था और वह अचानक भरभराकर उस पर गिर पड़ी है। वह प्रत्येक क्षण अपने को विश्वास दिलाता रहा कि नहीं, उसके व्यक्तित्व के शीशे में कोई दरार नहीं आयी है, पर उसे अन्तरतम में ऐसा लग रहा था कि वह शीशा टुकड़ा-टुकड़ा हो चुका है कि यदि उसे डैने के हल्केपन के साथ भी छू लिया गया, तो वह विखर उठेगा। "5 ऐसा ही एक और उदाहरण देखने को मिलता है- "सचमुच लोगों ने उसके बारे में अब तक न जाने क्या-क्या और कैसी-कैसी धारणाएँ बना ली होंगी। कल यदि वह गोपा से विवाह कर लेता है, तो लोग उसके बारे में और भी न जाने कैसी-कैसी धारणाएँ बना लेंगे और महिम हाहाकार से भर उठा।"6 आधुनिकता अभी भी हमारा मुखौटा है, वह हमारे रक्त में नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि हम मौखिक रूप में ही आधुनिक बातें करते हैं, किन्तु उन्हें व्यवहार में नहीं ला पाते। हमारा परिवेश, हमारी सामाजिक मान्यताएँ वाह्य तौर पर कितनी ही परिवर्तित क्यों न हों य किन्तु अभी भी बहुत कुछ है, जो बिल्कुल ही समय-निरपेक्ष है। तभी तो महिम कहता है- "सम्बन्ध भावावेश से तो नहीं चला करते।"7 इस उपन्यास में नरेश मेहता ने गोपा एवं महिम के प्रणय-सम्बन्ध का चित्रण किया है। प्रणय-चित्रण की नवीनता इस बात में है कि गोपा और महिम एक-दूसरे को बहुत चाहते हैं, फिर भी वे आपस के सम्बन्ध सामान्य नहीं बना पाते। महिम अत्यधिक भावुक है, अतः गोपा के जारज होने की बात सुनकर वह विक्षिप्त-सा हो उठता है। गोपा अत्यन्त संवेदनशील है, अतः कुछ दिन उपरान्त जब पुनः महिम उसके समीप अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने हेतु जाता है, तो वह अस्वीकार कर देती है। गोपा कहती है- "क्योंकि मैं... प्रेम चाहूँगी... सुरक्षा, आश्वासन, सामाजिकता आदि नहीं।"8 इस उपन्यास के नायक महिम की अस्थिरता इस प्रेम सम्बन्ध को पूर्णता नहीं प्रदान कर पाती। महिम का परिचय गोपा से उसके जन्मदिन पर हुआ। महिम गोपा से बहुत प्रभावित होता है और उसकी ओर आकर्षित होता चला जाता है। प्रतिक्रिया-स्वरूप गोपा की भी प्रत्येक भंगिमा उसकी अभिव्यक्ति बनती चली गयी "जब मैं नहीं बोल रही हूँ तो क्या आवश्यक है कि आप बोलें ?.... बहुत कुछ बोलने से परे भी होता है महिम बाबू।" किन्तु इस निकटता के बावजूद गोपा का एक अंश महिम के लिए सर्वथा एक अज्ञात रहस्य बना रहा, जिसे उद्घाटित करते-करते गोपा स्वयं बन्द हो जाती है। यह रहस्य गोपा को भीतर ही भीतर एक असहनीय बोझ की भाँति दबाए रहता है और महिम द्वारा बार-बार कुरेदे जाने पर भी वह कह नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए इस मनोव्यथा को महिम के हाथ सौंपना अपनी देह को सौंपना है- "असल में अपने मन की व्यथा को सौंपना और अपनी देह को सौंपना दो थोड़े ही होता है महिम बाबू। "10 महिम के निकट रहकर भी वह सहज नहीं हो पाती। अपनी दृष्टि में वह एक प्रवेचना मात्र है, जिसका उद्घाटन कर देने पर शेष कुछ नहीं रहेगा क्योंकि "हम जो जीते हैं, वह कह नहीं पाते और जो कह रहे होते हैं, उस रूप में ग्रहण नहीं किए जाते।"। महिम जहां संबंधों को अभिव्यक्त करता है वहीं गोपा उस संबंध को गहराई से जी रही होती है। कहीं न कहीं उसका स्वाभिमान संबंधों की कोमलता और जटिलता पर हावी हो जाता है। और परिणाम यह होता है कि महिम के हृदय पर गोपा चोट करती चली जाती है। वह जानती होती है कि उसके व्यवहार से महिम आहत होगा, लेकिन फिर भी वह प्रतिकूल व्यवहार करती जाती है- "मैं जानती हूँ कि कुछ नहीं होना है... पर मैं क्या करूँ महिम बाबू? मैं प्रत्येक साक्षात को ऐसे अस्वीकार कर देना चाहती हूँ, जैसे वह मेरे निकट कभी था ही नहीं, आप नहीं जानते कि आप सहज हैं जबकि गोपा नहीं, जो कुछ है न यह सब, केवल प्रवंचना है। प्रवंचना का एक दिन उसके बाद फिर कई दिन... ऐसी अनन्त श्रृंखला महिम बाबू।" 12 गोपा की अनुभूति जैसे यह सच्चाई जानती है कि "प्रेम के नाम पर कुछ भी करना प्रवंचना है "13 गोपा स्वयं भी महिम को अन्तर्मन से प्रेम करती है, परन्तु उसे अपने व्यक्तित्व के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पाती है- "महिम बाबू! क्या आप किसी भी दिन समझ पाएँगे कि गोपा ने आपको... केवल आपको। "14 गोपा महिम के लिए एक ऐसा क्षितिज बन जाती है, जो दूर से एक दिखने वाले धरती-आकाश की तरह उसके निकट प्रतीत होती है, किन्तु जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, वह और भी दूर होता जाता है। फार्म में यद्यपि गोपा कितनी सहज और निकट प्रतीत होती है, किन्तु फिर भी वस्तुतः वह दूर ही है। गोपा महिम को और उसके प्रेम को समझ नहीं पाती, उसकी दृष्टि में उसके प्रति महिम का आकर्षण उसके माध्यम से वैभव की चमक-दमक के प्रति ही प्रतीत होता है- "इसलिए कि अभी आपके अवचेतन में अनेक बातों, चमक-दमक के प्रति, कोठियों-बग्धियों के लिए लालसा है। मैं इसको बुरा नहीं कहती। मेरे लिए ये वितृष्णा है, जबकि आपके लिए लालसा। मैं इन सबको अपने सन्दर्भ से काट फेंकना चाहती हूँ, जबकि मेरे सन्दर्भ में आपको लगता है कि ये प्राप्त किये जा सकते हैं। आप क्षमा करें महिम बाबू... मैं जानती हूँ कि यह लालसा सहज है। यू विल गेट इट... अपने स्वार्थ के लिए मैं आपकी लालसाओं को होम नहीं होने दूंगी। "15 गोपा अपने स्वाभिमान के कारण किसी सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हो पाती जिससे महिम के साथ उसके सम्बन्ध में दूरियाँ पैदा होती चली गईं। वह कहती है- "मैं भी आपसे सम्बन्ध अनुभव करती हूँ, पर उस सम्बन्ध के प्रतिफल-स्वरूप कोई मांग या अपेक्षा नहीं है। "16 गोपा के व्यवहार से महिम का मानसिक तनाव बढ़ जाता है। वह अकारण ही खिंचे-खिंचे व्यवहार से परेशान रहता है। वह गोपा के जन्मदिन पर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है- "पता नहीं कब से कहना चाहता रहा हूँ गोपा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ... पर नहीं जानता कि कभी तुम्हें इसका विश्वास भी हो सकेगा।"17 महिम उसके समक्ष अपना प्रेम पूरी तरह अभिव्यक्त कर देता है, लेकिन गोपा इस वास्तविकता से भागना चाहती है, क्योंकि उसके मन में एक संघर्ष है। वह नहीं चाहती कि वास्तविकता जाने बिना महिम कोई विशेष कदम उठा ले। इस समाज की विडंबना और दोहरे चरित्र को गोपा अधिक जानती है क्योंकि वह एक स्त्री है। उसके जन्म की सच्चाई को सुनने के बाद इस समाज में कोई भी उसे सहानुभूति और दया के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाएगा। वह कहती है कि "विना सब कुछ बताए मैं आपका प्रेम नहीं स्वीकार करूँगी। छले जाने की क्या यातना होती है, यह मैं जानती हूँ और मैं आपको नहीं छलूँगी... लौट जाइए महिम बाबू! मेरी ओर से कोई बन्धन नहीं रहा आप पर। "18 इस प्रकार इस प्रेम सम्बन्ध का अन्त होता चला जाता है। गोपा का व्यक्तित्व दया-युक्त प्रेम स्वीकार नहीं करना चाहताः "मैं नहीं जानती महिम बाबू कि मेरा क्या होगा। पर आप लौट जाइए, प्लीज, यू विल गो अवे ऐट वन्स, लेट मी बी एलोन एण्ड एलोन। "19 गोपा ने अपनी मनोव्यथा से मुक्ति पाकर महिम के लिए एक विषम संघर्ष खड़ा कर दिया और जब वह गोपा को स्वीकारने का निर्णय लेकर उसके पास जाता है, तब गोपा उसके प्यार को अस्वीकार कर देती है। संघर्षों में-से गुजरता मन इतना जटिल हो जाता है कि वह एक क्षण में कोई निर्णय नहीं ले पाता। इसी कारण प्रेम- गाथा का सुखान्त नहीं होता। इस ठोकर को गोपा का आवेश मात्र मानकर महिम फिर भी उसी को अंगीकार करने का निश्चय बनाए रखता है, किन्तु गोपा की औपचारिकता बढ़ती ही जाती है। महिम अपने प्रेम को अभिव्यक्ति करता है उसकी सफलता और असफलता को भी अभिव्यक्त करता है वहीं दूसरी तरफ गोपा उस प्रेम को जी रही होती है। कहने को वह यह जरूर कहती है "भूल जाइए उस अतीत को। विश्वास माने, मैं भूल चुकी हूँ। मैं तो इस क्षण को भी अगले क्षण में भूल जान्त्र चाहूँगी। "20 गोपा से हुआ परिचय, अनेक शामें, उसकी मुद्राएँ, गोपा के सामीप्य में फार्म पर बिताएँ गए वे दो दिन, जो उसके व्यक्तित्व का अपरिहार्य अंग बन गये थे, किन्तु वे सब आज सदा के लिए शेष हो गए। प्रथम फाल्गुन' के माध्यम से श्रीनरेश मेहता ने प्रेम के स्वरूप की व्याख्या की है। प्रेम समान स्तर पर होता है। प्रेम कोमल भाव जरूर है लेकिन यह दया, करुणा और सहानुभूति से भिन्न है। हमारे यहां आधुनिकता के आने से प्रेम संबंधों के बाह्य स्वरूप में तो बड़ा परिवर्तन आया है लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी विवाह के लिए धर्म, जाति और समाज अपने-अपने अर्थ रखते हैं। सन्दर्भ सूची:- 1. श्रोत्रिय, प्रभाकर, (सं०), श्रीनरेश मेहता रचनावली, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, 2014, खण्ड-1, पृ०सं०-87 2. शर्मा, राकेश (सं०), चैत्य पुरुष नरेश मेहता, श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, 2023, पृ०सं०- 29, 30 |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 6, Issue 1, January 2025 |
| Published On | 2025-01-27 |
| Cite This | इन्द्रधनुष के रंगों में बसी प्रेम कहानी - जगदीश - IJLRP Volume 6, Issue 1, January 2025. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

