
International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 6 Issue 4
April 2025
Indexing Partners
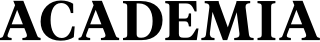




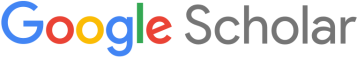













भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण
| Author(s) | पवन कुमार, डॉ. प्रज्ञान चौधरी |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है। उसका दमन भी उतना ही पाशविक और अभूत्पूर्व था। जिन परिस्थितियों में यह संघर्ष छेड़ा गया, वैसी प्रतिकूल स्थितियाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन में अब तक नहीं आई थीं। युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने को सख्त-से सख्त कानूनों से लैस कर लिया था और शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया था। पहली बात तो यह है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। नेहरू और गाँधी जैसे लोग भी थे, जो इस फासिस्ट-विरोधी युद्ध को किसी भी तरह कमज़्ाोर करना नहीं चाहते थे, इस निष्कर्ष पर पहुँच गए थे और अधिक चुप रहना यह स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है। ‘करो या मरो’ वाले अपने भाषण में भी गाँधीजी ने साफ-साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार बनना नहीं चाहता। लेकिन 1942 के वसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। क्रिप्स की वापसी के एक पखवाड़े बाद ही उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था तथा भारतीय जनता का आह्वान किया गया था कि जापान का हमला हो, तो वह अहिंसक असहयोग करे। नेहरू अगस्त तक संघर्ष के खिलाफ रहे, पर अंततः वे भी सहमत हो गए। संघर्ष अपरिहार्य इसलिए भी होता जा रहा था कि युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और ज़्ारूरी वस्तुओं के अभाव से जनसाधारण में बेहद असंतोष था। बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा उनके संभावित इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार द्वारा ज़्ाब्त कर लिया गया था, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही थी। सिंचाई की नहरों का कहीं जापानी ‘जल-परिवहन के लिए इस्तेमाल न कर लें, यह सोचकर नहरों का पानी बहा दिया गया, जिससे खेत सूखने लगे थे। मकानों और मोटर गाड़ियों पर भी सेना ने कब्ज़्ाा कर लिया था। जनता खुशी-खुशी युद्ध में शमिल होती, तो उसे यह सब नहीं अखरता, लेकिन यहाँ तो सब-कुछ उस पर लादा जा रहा था। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि ब्रिटेन की हार होने वाली है। दक्षिण-पूर्व एशिया से ब्रिटेन हट गया था और असम-बर्मा सीमा से आने वाली रेलगाड़ियाँ घायल सिपाहियों से भरी होती थीं। जब सिंगापुर और रंगून पर फाँसीवादी ताकतों का कब्ज़्ाा हो गया और कलकत्ता पर बम गिराए जाने लगे तो भगदड़ मच गई। 1942 के जून और जुलाई में 46 लोग जमशेदपुर से भाग गए और पूर्वी यू.पी. तथा बिहार से भागकर 50 हज़्ाार आदमी कानपुर पहुँचे। मलाया और स्थानीय लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया था। भारत के लोग सोचने लग गए थे कि अगर जापानी हमला हुआ तो अँग्रेज़्ा यहाँ भी उसी तरह विश्वासघात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष छेड़ने की ज़्ारूरत इसलिए भी महसूस हुई कि लोगों में निराशा फैल रही थी और यह आशा पैदा हो गई थी कि कहीं जापानी हमले का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध ही न हो। धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन में जनसाधारण की आस्था इतनी घट गई कि लोग बैंकों और डाकघरों से अपना रुपया निकालने लगे और अपनी बचत को सोने, चांदी और सिक्कों में बदल कर रखने लगे। पूर्वी संयुक्त प्रांत (यू.पी.) और बिहार में अनाज की जमाखोरी इतनी बढ़ गई कि बिहार के राज्यपाल स्टीवार्ट ने सरकार को लिखा कि चावल की कोई कमी नहीं है, पर वह बाज़्ाार में नहीं आएगा। सरकारी अधिग्रहण से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने जखीरों को बैंकों के पास बंधक रख दिया है। पता चला है कि उत्तर बिहार में बैंकों के पास बंधक अनाज उसका तीन गुना है, जितना इस मौसम में सामान्यतः रहता है। यों तो गाँधीजी आने वाले संघर्ष के बारे में चर्चा करते ही आ रहे थे, परन्तु अब देर करना उन्हें गलत लगने लगा था। उन्होंने कांग्रेस को यह चुनौती भी दे डाली कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूँगा। नतीज़्ातन कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा की अपनी बैठक (14 जुलाई 1942) में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होने वाली थी, जिसमें इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था। ऐतिहासिक सभा बंबई के ग्वालिया टैंक में हुई। जनता का उत्साह देखते ही बनता था। अंदर तो नेता विभिनन मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे थे और बाहर जनसमुद्र उमड़ रहा था। नेताओं का निर्णय जानने की उत्सुकता इतनी थी कि खुले अधिवेशन में जब भाषण होने लगे, तो हज़्ाारों-हज़्ाार की भीड़ होने के बावजूद सभा में पूरी शांति थी। |
| Keywords | - |
| Published In | Volume 4, Issue 7, July 2023 |
| Published On | 2023-07-05 |
| Cite This | भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण - पवन कुमार, डॉ. प्रज्ञान चौधरी - IJLRP Volume 4, Issue 7, July 2023. |
Share this


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

